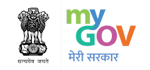मंदिर की वास्तुकला
मौर्य शासक अपनी कला और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे । उत्खनन के दौरान प्राचीन मंदिरों के अवशेष सामने आए हैं । राजस्थान में जयपुर के बैराट जिले में ईसा पूर्व 3 शताब्दी का एक मौर्यकालीन गोलाकार ईंट और इमारती लकड़ी का मंदिर मिला है । तेईस मीटर व्यास का यह मंदिर चूने से पलस्तर की गई ईंटों का बना था जिसके एकांतर में लकड़ी के 26 अष्टभुजाकार स्तंभ थे । इसका प्रवेश पूर्व दिशा में एक छोटी डयोढ़ी से था जो लकड़ी के दो स्तंभो पर टिकी थी और इसके इर्द-गिर्द सात फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था । उत्खनन के दौरान मिला एक अन्य मौर्य मंदिर, सांची में मंदिर 40 की योजना भी उपरोक्त मंदिर से मिलती-जुलती है । पत्थर से बने इस मंदिर की अर्द्धवृत्ताकार योजना में इस मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ था और यह मंदिर एक ऊँचे आयताकार अनुमाप पर निर्मित था और इसमें प्रवेश विकर्णत: विपरीत छोरों पर बनी सोपान पंक्ति से संभव था । संभवत: लकड़ी से बनी अधिरचना अब विलुप्त हो चुकी है । आगामी शताब्दियों में मंदिर में अनेक परिवर्तन हुए जिसके कारण इसे मूल रूपरेखा के माध्यम से पहचानना कठिन हो गया ।
सांची में मंदिर 18 भी पत्थर से बना एक अर्द्धवृत्ताकार मंदिर था जिसकी अधिरचना संभवत: इमारती लकड़ी से की गई थी । यह मंदिर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है । भव्य स्तंभों और भित्ति स्तंभों वाले अर्द्धवृत्ताकार मंदिर के वर्तमान अवशेष 7वीं शताब्दी ईसवी सन् के हैं, हालांकि इस मंदिर में मध्य काल तक पूजा अर्चना की जाती थी ।
संभवत: अपने मूल रूप में जो प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर आज भी खड़ा है वह कर्नाटक में ऐहोल में है । यह एक छोटा सा ढांचा है जो विशाल, शिलाखंड के समान पत्थर के खंडों से बना है । मंदिर में गर्भगृह या एक आम चौकोर कक्ष है जिसके सामने एक आच्छादित बरामदा और एक ड्योढ़ी है जिसमें पत्थर की छत को सहारा देते चार भारी स्तंभ हैं । स्तंभ और पूरा ढांचा अत्यंत साधारण हैं सिवाय मुंडेर पर बनी एक छोटी सी चित्रवल्लरी के जो ड्योढ़ी के दोनों ओर ज़मीन पर बनी है ।
रोचक बात यह है कि जिस वास्तुकार ने इस इमारत का निर्माण किया उसे तब तक इस बात का ज्ञान नहीं था कि कक्ष के निकटतम दो स्तंभों को दीवार से अलग खड़ा करने के स्थान पर उन्हें भित्ति स्तंभ, अर्द्ध स्तंभ या बरामदे के पीछे की दीवार से आधा निकला हुआ बनाया जा सकता था । न ही उसने मौसम का ध्यान रखा और न ही छत पर से बहने वाले वर्षा के पानी के लिए परनालों का प्रावधान रखा । यह पूरा ढांचा भारी, विशाल और बेढंगा है । इसका निर्माण संभवत: सन् 300 से 350 ईसवी में किया गया था ।
सांची में मंदिर संख्या 17 सन् 400 ईसवी में निर्मित एक छोटा सा मंदिर है और पहले बनाई गई प्रत्येक वस्तु का यहां बेहतर प्रकार से निर्माण किया गया है । पत्थरों का आकार छोटा है और उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से निर्धारित पंक्तियों में लगाया गया है । छत को अलग कर दिया गया है ताकि डयोढ़ी की ऊँचाई गर्भ गृह की तुलना में कम हो क्योंकि गर्भ गृह ही भगवान का मुख्य मंदिर था । बारिश के पानी की निकासी के लिए सोच समझकर परनाले बनाए गए हैं और पिछले चार स्तंभ अधिक पतले और सुंदर नक्काशी के साथ हैं । यह मंदिर वास्तव में प्राचीन काल का है और इसमें लालित्य, सामंजस्य, संतुलन और भव्यता का मेल है । सजावट न्यूनतम है और इसका प्रयोग केवल एक संरचनात्मक ढांचे को दूसरे से जोड़ने के स्थान पर एक औंधा कमल रखा गया है । जहां पर छत स्तंभ के ऊपर टिकी है वहां पर शीर्ष और सिंहों की आसीन आकृतियां पीछे से जुड़ी होने के कारण सहारे के काम करती हैं । संपूर्ण ढांचा सरल और जटिलता रहित है । लेकिन समय के साथ अत्यंत सरल और अनलंकृत मंदिर की वास्तुकला धीरे-धीरे जटिल हो जाती है । सरल चतुष्कोण धीरे-धीरे प्रमुख और पुन: प्रवेश होने वाले कोणों में विकसित हो जाता है, उदवर्तन जोड़े जाते हैं जिससे रूपरेखा और स्पष्ट हो जाती है जब तक कि वह लगभग एक तारे के समान नहीं लगने लगती जिसमें ज़मीनी स्तर पर सौ से अधिक छोटे-छोटे कोण होते हैं ।
ऐहोल का लड़खन मंदिर 5 शताब्दी ईसवी का है । यहां पर वास्तुकार के प्रदक्षिणा पथ पर ध्यान देने का प्रयास किया है जो कि चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ है जिससे भक्त पवित्र आत्माओं की प्रदक्षिणा कर पाते हैं । वास्तव में जब बड़ी संख्या में भक्त एक अंधेरे गलियारे में घूम रहे होते हैं तब प्रकाश और वायुसंचार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वास्तुकार ने छिद्रित जालियां बनाई हैं । इस इमारत में प्रवेश द्वारा की डयोढ़ी अपेक्षाकृत छोटी रखी गई है और इस पर अधिक ज़ोर नहीं दिया गया है । वास्तव में यह केवल प्रवेश द्वार ही है । यह इमारत अब भी हमें लकड़ी के एक आदिप्रारूप की याद दिलाती है जिसकी पत्थर की दीवारें ढलावदार छत को सहारा देती हैं जो पत्थर की पट्टियों से बने विशाल शिलाखंडों से निर्मित है । अत्यंत बुद्विमानी से छत को ढलावदार बनाकर उसमें परनाले बनाए गए हैं ताकि बारिश के पानी की अच्छी तरह से निकासी हो सके । गर्भगृह की छत थोड़ी ऊँची रखी गई है और यह सही भी है क्योंकि यह भगवान का निवास स्थान है । इस इमारत के ऊपर पहली बार बुर्ज बनाने का प्रयास किया गया है जो भविष्य के विशाल शिखर का पूर्वगामी है । इसके पीछे जो मूल कारण था वह यह था कि मंदिर देवताओं का निवास स्थान है, इसलिए दूर और पास, गांव और नगर के विभिन्न हिस्सों से इसे दिखना चाहिए । इस कारण इसे इर्द-गिर्द की इमारतों से ऊँचा और विशाल बनाया जाता था ।
सन् 550 ईसवी में निर्मित ऐहोल का दुर्गा मंदिर अर्द्धवृत्ताकार है जिसमें वास्तुकार ने अपने विगत प्रयासों की अपेक्षाकृत अनेक परिवर्तन किए हैं । इस मंदिर में एक ऊँचा मंच है और लड़खन मंदिर की भांति एक अंधेरे प्रदक्षिणा पथ के स्थान पर यहां पर स्तंभों पर टिका एक खुला बरामदा है जो कि प्रदक्षिणा पथ का काम करता है । छिद्रित जालियों के स्थान पर यहां मंदिर के इर्द-गिर्द स्तंभों वाला बरामदा है जो खुला, हवादार और रोशन है । विशाल प्रवेशद्वार की सीढि़यां ऊँचे आधार तक जाती हैं । छत की ऊँचाई लगभग दुगुनी है और इस इमारत में बुर्ज एक छोटे शिखर का आकार लेने लगा है जो आगामी शताब्दियों में एक ऊँचे शिखर में परिवर्तित हो गया । ये स्तंभ अत्यंत अरुचिकर लगते यदि शिल्पकारों को इनपर सुंदर प्रतिमाएं न उकेरने दी गई होतीं । स्तंभों की पंक्ति के नीचे भी नक्काशी की गई है और पहली बार हमें मंदिर के चौड़े प्रवेश के पार शहतीर को सहारा देने वाले ब्रैकेट दिखाई पड़े । इसे देखकर हमें पुन: लकड़ी प्रयोग करने वालो वास्तुकार का आभास होता है जो कि बांस या लकड़ी के स्तंभों को खड़ा कर उनपर समस्तर पर कडि़यां डालता था ताकि छत अपने स्थान पर टिकी रहे । इस निर्माण को दुगुनी मज़बूती देने के लिए उसे ब्रैकेट बनाने का विचार आया जो कि भारत में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक प्रमुख अवयव है । इसे बहुत पहले चीन में प्रयोग किया जाता था जिसमें पत्थर का एक तिरछा टुकड़ा स्तंभों से निकलकर सरदल या कड़ी को मजबूती से पकड़ता था । इस प्रकार के निर्माण को वास्तुकला में क्षैतिज कहते हैं जो मेहराबदार से भिन्न है । क्षैतिज निर्माण पद्धति का बाद में मुसलमानों ने प्रयोग किया ।
संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काट कर बनाए गए थे । ये मंदिर मद्रास के दक्षिण में 38 मील दूर समुद्र तट पर 5वीं शताब्दी ईसवी में बनाए गए थे । स्थानीय भाषा में इन्हें रथ कहते हैं और इनका नाम पांच पांडव भाइयों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है हालांकि न ही इनका रथ और न ही पांडवों से कुछ लेना-देना है और यह संबंध पूर्णत: स्थानीय है । कांचीपुरम के महान पल्लव शासकों ने अनेक निर्माण किए और पल्लव शिल्पियों ने समुद्र तट पर उपलब्ध चट्टानों और शिलाखंडों का प्रयोग कर उन्हें मंदिरों (अखंडित) तथा छोटे शिलाखंडों को काटकर उनसे सिंह, हाथी, वृषभ इत्यादि की विशाल मूर्तियों को आकार दिया ।
चट्टानों से काटकर बनाए गए इनमें से एक मंदिर को द्रौपदी रथ कहा जाता है । यह लकड़ी के स्तंभों के सहारे खड़ी छप्पर की छत वाली मिट्टी की झोपड़ी की पत्थर पर अनुकृति है । द्रोपदी रथ में एक चौकोर कक्ष है लेकिन डयोढ़ी नहीं है और इसकी छत अपने आकार से बंगाली झोपड़ी का आभास देती है । हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कई कारण हैं कि भारत में संरचनात्मक वास्तुकला के विभिन्न प्रकारों की भांति यह भी बांस और छप्पर से निर्माण के आदिप्रारूप की अनुकृति है । प्रवेशद्वार पर दो सुंदर लड़कियों की आकृतियां हैं, प्रत्येक को प्रवेशद्वार के दोनों ओर बनाए गए छोटे से आले में तराशा गया है । इन के किनारों पर पुष्पों से सजावट की गई है जो कुछ लोगों के अनुसार छप्पर को अपने स्थान पर रखने के लिए मूल रूप से बनाए गए पीतल और तांबे के किनारों की चट्टानों पर अनुकृति है ।
आकार और देखने में बाकी के रथ ऐसा आभास देते हैं मानों वे एक चौकोर प्रांगण के इर्द-गिर्द कक्षों वाली इमारत में विकसित हुए हैं । जैसे-जैसे मठ में रहने वाले भिक्षुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई, एक-एक करके इमारत में मंजिलें जोड़ी गईं और अंत में इमारत के ऊपर एक गुंबदाकार छत का निर्माण किया गया । इनकी रूपरेखा चौकोर है और इनके ऊपर पिरामिडी शिखर बना है जैसे कि अर्जुन का रथ और धर्मराज रथ ।
एक अन्य प्रकार के रथ की लंबी और बेलनाकार मेहराबी छत है, यानि की हाथी की पीठ (गजपृष्ठकर) की भांति । ऐहोल का दुर्गा मंदिर और भुवनेश्वर का वैताल देउल इसके उदाहरण हैं । चौकोर मंदिरों में छत अनेक झोंपडियों की छतो की भांति है जो कि काफी कुछ बौद्ध स्मारकों और अन्य छोटी झोंपडियों में दिखाई देता है । हालांकि इन्हें पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया है लेकिन तथाकथित बुद्ध के छोटे से सिर के साथ ये एक बौद्ध चैत्य झरोखे का आभास देती हैं । अर्जुन का रथ और धर्मराज रथ का बेहतरीन अनुपात, रोशनी और छाया का विन्यास इनके शास्त्रीय स्वरूप की ओर संकेत करता है । साधारण, ऊर्ध्वाधर स्तंभों की अनुकृति के सहारे दीवारगीर टिके हैं और भित्ति स्तंभों के तल पशु आकार में बने हैं । जहां सांची में पशुओं का शीर्ष के स्थान पर प्रयोग किया गया था वहीं यहां पर उनका आधार के रूप में प्रयोग किया गया है ।
जुड़वाँ भाइयों, नकुल और सहदेव, के नाम पर बना एक मंदिर अर्द्धवृत्ताकार है जिसे धर्मराज, अर्जुन और अन्य रथों की भांति अलंकृत किया गया है । छत का आगे की ओर थोड़ा विस्तार कर एक डयोढ़ी बनाई गई है जिसे दो सिंह स्तंभ सहारा दे रहे हैं । इस मंदिर में कोई आकृतियां उत्कीर्ण नहीं की गई हैं । इसके समीप एक एकाश्मक हाथी है जो अर्द्धवृत्ताकार मंदिर के हाथी की पीठ (गजपृष्ठकर) आकार की ओर संकेत करता है ।
महाबलीपुरम का गणेश रथ, उत्कृष्ट एकाश्मक मंदिरों में से एक है । हालांकि यह तीन मंजिला है और इसमें बेहतर कारीगरी है, लेकिन इसकी छत भीम रथ की भांति है । चौपहिया गाड़ी समान छत के त्रि-अंकी छोरों पर स्थापित कलश पर रखे मानव सिर को त्रिशूल रूपी शिरोवस्त्र से सुसज्जित किया गया है जिसमें बाहर की ओर के कांटे आमतौर पर द्वारपाल की मूर्तियों के सींग की ओर संकेत करते हैं और मध्य का कांटा लंबे और संकुचित मुकुट की ओर । यह चिह्न चौपहिया गाड़ी के आकार वाली छत के कलश के सज्जित त्रिअंकों में बार-बार आता है । इसके अलावा मंडप और कुडु अलंकरण तो है ही । विस्तृत रूप से अलंकृत छत पर फूलदान के आकार के नौ कलश हैं और यह भावी गोपुरम का अग्रगामी है । दोनों किनारे और पृष्ठभाग भित्ति स्तंभों की पंक्ति से सुसज्जित हैं जबकि मुख्य प्रवेश पश्चिम की ओर है । दोनों छोरों पर द्वारपाल के बीच दो सिंह स्तंभ और दो भित्ति स्तंभ हैं ।
समुद्र तट पर स्थित महाबलीपुरम् का मंदिर उत्तर 7वीं शताब्दी का है । यह मंदिर विशेष रूप से समुद्र तट पर अपनी अवस्थिति के लिए जाना जाता है । हालांकि शैलीगत रूप से यह मंदिर धर्मराज रथ के काफी समान है लेकिन इसमें एक प्रमुख भिन्नता भी है । यह मंदिर शैलोत्कीर्ण न होकर मूर्तिमय है । यह धर्मराज रथ से तीन से चार गुणा विशाल है और इसके पृष्ठभाग में मंदिर को जोड़कर इसे तिगुनी इमारत बनाया गया है जो थोड़ा बाहर की ओर निकली है । इसमें दो शिखर हैं जो पहले के मंदिरों से ज्यादा विशाल हैं । दोनों शिखरों में से ज्यादा ऊँचे शिखर में धर्मराज रथ से अधिक मंजिलें हैं । और इसकी चौटी ऊँची और नोकदार है । यह कहीं अधिक जटिल, विशाल और अलंकृत है । मंदिर के इर्द-गिर्द एक विशाल दीवार है जिसमें निर्धारित दूरी पर सिंह के भित्ति स्तंभ वाला पल्लव शैली का परकोटा है । इसकी बाहरी ओर दीवार पर बैठी हुई वृषभ आकृतियां हैं ।
आठवीं शताब्दी ईसवी में समुद्र तट पर स्थित महाबलीपुरम् के मंदिर के निर्माण के पश्चात् राज सिम्ह ने कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया । महाबलीपुरम् के मंदिर की तुलना में कैलाशनाथ मंदिर आकार में अधिक विशाल और दिखने में ज्यादा भव्य है । एक आयताकार प्रांगण में स्थित कैलाशनाथ मंदिर रथ जैसे दिखने वाले प्रकोष्ठों की अविरल शृंखला से बना है जो परिस्तंभों से घिरा हुआ है । यहां की पल्लव शैली और अधिक परिष्कृत और अलंकृत है । इसमें शामिल हैं गर्भ-गृह, मंडप, प्रदक्षिणा पथ और एक विशाल कक्ष के आकार में एक डयोढ़ी । समतल छत और स्तंभों वाला मंडप, जो मूल रूप से एक अलग इमारत था, एक डयोढ़ी द्वारा गर्भ-गृह से जुड़ा हुआ था ।
इस मंदिर का एक दिलचस्प पक्ष गर्भ-गृह के तीन ओर बने पूजा स्थल हैं । लालित्यपूर्ण परिरेखा वाले पिरामिडी बुर्ज में अनेक मंजिलें हैं जिसमें प्रत्येक में भारी छज्जे और स्तूपिक हैं । शिखर का अनुपात समान और ठोस होने के साथ इसके आकार में लयात्मकता और रूपरेखा सुरुचिपूर्ण है ।
सारनाथ का धमेख स्तूप एक भव्य गुप्तकालीन बेलनाकार इमारत है (ऊँचाई 43.5 मीटर, धरातल का व्यास 28.3 मीटर) जो कि पत्थर और ईंट से बनी है । इसके पत्थर के तहखाने में आठ बहिर्विष्ट अग्रभाग हैं जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए विशाल आले बने हुए हैं । इसके अलावा इसे बारीकी से उत्कीर्ण पुष्प और ज्यामितीय रचना से अलंकृत किया गया है । बुद्ध के ज्ञानोदय के पवित्र स्थल के रूप में यहां पर अनेक मंदिर, स्तूप और मठ फले-फूले । परंपरानुसार ज्ञानोदय के पूर्व और बाद की घटनाओं की स्मृति में इस स्थान पर अनेक मंदिर और स्मारक बनाए गए ।
ईंटों से निर्मित मुख्य पूजा-स्थल जिसे महाबोधि मंदिर कहते हैं का निर्माण लगभग दूसरी शताब्दी ईसवी में हुआ था लेकिन लगभग 14वीं शताब्दी ईसवी में पुनरुद्धार के नाम पर इसके चार कोनों पर भारी बुर्जों का बोझ डाल दिया गया । इसके बीचों-बीच एक ऊँचे मंच पर खड़ा बुर्ज 55 मीटर और सात मंजिला ऊॅंचा सीधे किनारों वाला पिरामिड है जो कि भित्ति स्तंभों और चैत्यों में बने आलों से जुड़ा हुआ है ।
साहित्यिक परंपरानुसार राजगीर से 10 किलोमीटर उत्तर में प्राचीन नगर नालंदा में बुद्ध और महावीर आए । माना जाता है कि अशोक ने बुद्ध के अनुयायी, सारिपुत्त के चैत्य आलों में पूजा की ओर एक मंदिर की स्थापना की । हर्ष के काल तक नालंदा, महायान शिक्षा का एक मंदिर की स्थापना की । हर्ष के काल तक नालंदा, महायान शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र और एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नगर बन गया था जिसमें अनेक पवित्र स्थल और मठ थे जहां दूर-दूर से विद्वान आते थे । चीनी तीर्थयात्री हवेनत्सांग और फ़ाहियान ने नालंदा में अध्ययन किया और वहां रहने वाले लोगों और जीवन का वृत्तांत लिखा ।
मंदिर संख्या 3, 31 मीटर से भी ऊँचा था और इसमें एक के बाद एक सात समूह थे जिसमें से हाल के दो 11वीं और 12वीं शताब्दियों से थे और पांचवां , जो लगभग छठीं शताब्दी का था, अपनी प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था । मठ भव्य आयताकार इमारतें थीं जिनमें से प्रत्येक में एक खुला प्रांगण और इर्द-गिर्द ढका हुआ बरामदा था जो चारों ओर बने प्रकोष्ठों की आरे ले जाता था । प्रवेश द्वारा के सामने वाले प्रकोष्ठ को पूजा स्थल मानते थे । नालंदा, पाल प्रतिमाओं और कांस्य प्रतिमाओं का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र था और यहां से अत्यंत ऐतिहासिक महत्त्व की मुहरें और मुहरबंदी मिली हैं ।
आइए अब हम एक ऐसे क्षेत्र पर दृष्टि डालें जहां मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली का एक दिलचस्प दिशा में विकास हुआ ।
छठी शताब्दी ईसवी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की शैली लगभग समान थी । लेकिन छठी शताब्दी ईसवी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न-भिन्न दिशाओं में विकास हुआ । वर्तमान के लिए हम यह मान कर चलते हैं कि दो क्षेत्र जहां मंदिर वास्तुकला स्पष्ट रूप से विकसित हुई वे थे दक्कन और ओड़ीशा और इन दोनों ही क्षेत्रों मं उत्तर और दक्षिणी शैली के मंदिर साथ-साथ पाए जा सकते हैं । ओड़िशा में विमान, मुख्य पूजा-स्थल पर मंदिर का बुर्ज, भारत में वास्तुकला के भव्यतम आविष्कारों में से एक है और दक्षिण भारतीय गोपुरम की तुलना में क्रियात्मक दृष्टि से कहीं अधिक परिष्कृत है । दक्षिण भारत में गोपुरम में बेलनाकार बुर्ज गर्भ गृह के ऊपर न होकर केवल एक महिमामंडित प्रवेशद्वार है । अपनी भूमिका में हमने इस बात की ओर संकेत किया था कि वास्तुकार मंदिर को इर्द-गिर्द की अन्य इमारतों से अधिक महत्व देना चाहता था क्योंकि यहां उसके देवता का गर्भ-गृह में निवास था । ओड़ीशा में शिखर अपने विशाल और भव्य आकार से दूर-दूर तक भगवान की उपस्थिति दर्शाता है जैसा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर या भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से विदित है जो भक्तों के ह्रदय में सम्मान का संचार करते हैं और यहां आने वाले सभी को प्रभावित करते हैं । मंदिर का शिखर या विमान, जैसा कि इसे ओड़ीशा में कहा जाता है, लोगों की धार्मिक भावनाओं का सशक्त उदगार था । यहां पर दर्शाए गए भुवनेश्वर के वैताल देउल मंदिर का अध्ययन दिलचस्प होगा जो कि आठवीं शताब्दी ईसवी में शक्ति पंथ का ढोलाकार आकृति वाला मंदिर है । मंदिर का अग्रभाग या बाहरी हिस्सा पट्टी जैसी आकृतियों द्वारा विभाजित हैं जो ढोलाकार छत से धरातल तक जाता है । ये पट्टियां थोड़ा सा बाहर की ओर निकली हुई हैं और इनमें बने आलों में मूर्तियां रखी हुई हैं । वास्तविक ढोलाकार छत अत्यंत अलंकृत और क्रमानुसार कम होते एक दूसरी के ऊपर रखे ढांचों पर टिकी हुई है । ढोलाकार छत प्राचीन झोपड़ी की छप्पर वाली छत की पत्थर पर अनुकृति है । छप्पर की यह छत अत्यंत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में भी बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों में देखी जा सकती है ।
यहां याद रखने लायक दिलचस्प बात यह है कि पुरातन काल की गरिमामय सादगी और सौहार्द्र से विस्तृति, जटिलता और आलंकारिक सजावट की ओर विकास में एक निश्चित नमूना देखने को मिलता है जो कि सांची के मंदिर में देखा गया है जहां सादगी और सौहार्द्रता का स्थान बढ़ते हुए अलंकरण और सजावट ने ले लिया है ।
जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, भारत में मूर्तिकार और वास्तुकार अक्सर एक ही व्यक्ति होता था और इसलिए मूर्तिकला और वास्तुकला को अलग-अलग देखना एक भूल होगी । वास्तव में मूर्तियों का प्रयोग मंदिर के अग्रभाग की बाहरी दीवारों को अलंकृत करने के लिए किया जाता था । आइए, एक बार पुन: 5वीं शताब्दी के महान सांची के मंदिर पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि यह इमारत कितनी साधारण और इसकी दीवारें कितनी खाली और अनलंकृत हैं । इसके बाद आपने देखा होगा कि 5वीं शताब्दी की मध्य में लड़खन मंदिर की दीवारों पर जालीदार खिड़कियां बनाकर कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया गया । लगभग 100 वर्ष बाद ऐहोल के दुर्गा मंदिर में बरामदे के इर्द-गिर्द स्तंभों पर मूर्तियां बनाई गईं । सातवीं शताब्दी के आरंभ में धीरे-धीरे वैताल देउल में भी पट्टियों जैसे बहिर्वेशन में आलों का अत्यधिक प्रयोग कर मंदिर को अलंकृत किया और सजाया है ।
1000 ईसवी तक मंदिर को सजावटी तत्वों से अलंकृत किया गया । भुवनेश्वर का राज रानी मंदिर अत्यंत सुसज्जित है । इसमें यक्षी आकृति विलासमय प्राकृतिक वातावरण में खड़ी हुई हैं ।
प्राचीन भारतीय मंदिर की छत सपाट थी और इसमें एकत्रित वर्षा के जल की निकासी की समस्या थी । ऐहोल में लड़खन और दुर्गा मंदिरों में छत पर लगाई गई पटियों को ढलान दी गई है । मध्य 7वीं शताब्दी में ओड़िशा में भुवनेश्वर के परशुरामेश्वर मंदिर में विशाल पत्थरों की पटिया लगाई गई थीं । इस मंदिर में ढलावदार पटिया की एक के ऊपर एक, दो छतें थीं जिनमें बने छोटे-छोटे इरोखों से मंदिर के भीतर प्रकाश बिखरता था । ढलावदान पटिया वाली ये छतें धीरे-धीरे एक से बढ़कर दो और दो से बढ़कर तीन हो गईं और इन छतों को बढ़ाकर वेदी के ऊपर एक पिरामिडी छत बनाई गई जिसे ओडिशा में जगमोहन कहते हैं और यह मुख्य पूजा-स्थल से पहले है ।
भुवनेश्वर का राजरानी मंदिर भारतीय वास्तुकला की श्रेष्ठ कृति है । उत्कृष्ट लालित्य से परिपूर्ण इस मंदिर में जगमोहन और विमान के आकार को साथ लाकर पूर्णता दर्शाई गई है । ज़मीन से उठता हुआ छत्ते के आकार को एक मीनार गर्भ-गृह के ऊपर जाकर धीरे से मुड़ जाती है । शिखर पर शिखर, एक के ऊपर एक मंदिर की लघु मीनारों की ऊँचाई विशाल एवरेस्ट पहाड़ के समान बढ़ती जाती है जो छोटे-छोटे शृंगो से घिरा हुआ है । संभवत: ऊपर की ओर बढ़ते हुए वास्तुकार ने इन लघु शिखरों के बारे में सोचा और उसे महान पर्वत शृंखला और हिमालय की सबसे ऊँची चोटी से प्रेरणा मिली जो कि छोटी-छोटी चोटियों से घिरा हुआ है अथवा यह मनुष्य की आत्मा के ऊपर तक पहुँचकर शाश्वत और सर्वशक्तिमान आत्मा से मिलने और उसमें लीन होने का प्रतीक था ।ओडि़शा के ये मंदिर वास्तुकारों और शासकों के अत्यंत धैर्य, स्नेहपूर्ण रखरखाव और अध्यवसाय का प्रतीक हैं जिसके चलते उन्होंने जगमोहन अथवा मंडप के ऊपर साधारण ऊँचाई की अत्यंत साधारण पिरामिडी छत के स्थान पर अलंकरण किया । ढलावदार पटिया का बाहुल्य 13 समतल अवयवों में नज़र आता है जो कि पिरामिड के शिखर की ओर बढ़ते हुए घटता जाता है लेकिन सुंदर गोल पत्थर, अम्लयक, छत्र या शिखर के ऊपर किरीट के महत्त्व के समक्ष यह शिखर भी छोटा लगने लगता है । जगमोहन और विमान, जगमोहन की पिरामिडी छत से उभरने वाले लघु शिखर, जो कि गर्भ गृह के शिखर जक जाते हैं, के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिससे परिवर्तन एक कदम की भांति लगता है जो आपकी दृष्टि को शिखर की ऊँचाई तक ले जाता है ।
हमने देखा कि ओड़िशा में मंदिर वास्तुकला के विकास में योजना के विस्तार और बाहरी दीवारों पर अत्यधिक अलंकरण पर ज़ोर है । यहां पर मंदिरों को सजावटी तत्व, मानव आकृतियों, देवी-देवताओं और पशु-पक्षियों से अलंकृत किया गया है । साधारण आकार के प्रारंभिक काल के मंदिरों के शिखर अपेक्षाकृत छोटे थे । उदाहरण के लिए भुवनेश्वर में मध्य 7वीं शताब्दी का परशुरामेश्वर मंदिर जिसके आधार और गर्भ गृह के ऊपर भारी शिखर और नीची सपाट छत वाला मंडप सुंदर नर्तक और नर्तकियों तथा वाद्यकारों की मूर्तियों से अलंकृत है, धीरे-धीरे एक अत्यंत ऊँची और विशाल इमारत में परिवर्तित हो जाता है जिसे मूर्तियों से सजाया गया है । इसके बाद 8वीं शताब्दी के अंत में वैताल देउल मंदिर आता है जो अपनी मूर्तियों के लालित्य और प्रचुर सजावट के लिए जाना जाता है । इस मंदिर का आयताकार गर्भ-गृह और चौपहिया गाड़ी के समान छत परशुरामेश्वर मंदिर की भांति है । इसका काल निर्धारण इसके सजावटी तत्वों और रूपरेखा के आधार पर आठवीं शताब्दी के अंत में किया जा सकता है । इसके सजावटी तत्त्व और रूपरेखा परिपक्व, अर्थपूर्ण और गतिशील हैं । इसके बाद मुक्तेश्वर मंदिर आता है जिसे ओड़ीशी वास्तुकला का रत्न माना जाता है ।
ब्रह्मेश्वर मंदिर एक पंचायतन मंदिर है जिसका निश्चित काल निर्धारण एक शिलालेख द्वारा सन् 1060 ईसवी में किया जा सकता है । इस मंदिर में केंद्रीय पूजा स्थल के इर्द-गिर्द अहाते के चार कोनों में चार छोटे पूजा-स्थल हैं । हालांकि यह एक अत्यंत सुंदर पूजा-स्थल है लेकिन इसका शिखर अचानक ही अम्लक के नीचे मुड़ा हुआ प्रतीत होता है । वहीं दूसरी ओर राजरानी का शिखर शैली और सजावट की दृष्टि से आदर्श और उत्कृष्ट है । जगमोहन की छत काफी भारी और पिरामिडी आकार की है जबकि राजरानी की छत मामूली ऊँची और साधारण है ।
वास्तुशिल्पीय गतिविधियों की पराकाष्ठा सन् 1000 ईसवी में निर्मित भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में देखी जा सकती है जो संभवत: इस शताब्दी का सबसे उत्कृष्ट, भव्य और विशालतम (36.50 मीटर ऊँचा) मंदिर है । इस मंदिर में गर्भ-गृह विशाल बंद कक्ष, नृत्य कक्ष और भेंट अर्पित करने के लिए कक्ष हैं जिनमें से अंतिम दो को बाद में जोड़ा गया । लिंगराज के इर्द-गिर्द अतिरिक्त पूजा स्थल हैं जिनसे पूरा अहाता अस्त-व्यस्त हो गया है । इसके शिखर की ऊँचाई राजरानी से पांच गुना अधिक है । संपूर्ण परिसर में इसकी भव्यता और विशाल आकार रथों की गहरी सीधी रेखाओं के कारण और मुखर हो जाता है । केंद्रीय रथ के दोनों ओर दो ऐसी रेखाएं हैं जिनमें शिखर के आकार में चार अवरोहात्मक अनुकृतियां हैं । भव्यता में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए जगमोहन और शिखर भगवान का महात्म्य दर्शाते हैं । जगमोहन की नौ निचली छतें और सात ऊपरी छतों को पैदल सेना, घुड़सवार फ़ौज, हाथी व अन्य दृष्य दर्शाती चित्रवल्लरी से अलंकृत किया गया है जो ऊपर की ओर उठते पिरामिड की एकरसता को तोड़ते हैं । इसके अलावा एक महान शिखर सतह के लालित्य में, कोने में लघु शिखर और उडते हुए शेर बनाकर भिन्नता प्रदान करने का प्रयास किया गया है । मंदिर पर उकेरी गई स्त्रियों की लालित्यपूर्ण और सुंदर आकृतियां, एक दूसरे के पाश में प्रेमी युगल और अन्य देवी-देवताओं को ऐंद्रिय आकर्षण, सुंदरता और उत्कृष्ट आकार में उकेरा गया है । संपूर्ण इमारत की परिपक्व योजना, विभिन्न हिस्सों का संतुलित वितरण, शिखर का लालित्यपूर्ण घुमाव और मनोहर और सुघट्य अलंकरण के साथ इसके प्रभावशाली आयाम भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर को भारतीय वास्तुकला की महानतम कृति बना देते हैं । तकनीक की दृष्टि से गढ़े गए पत्थर से इतने विशाल आकार का शिखर और पूजा स्थल बनाना वास्तुकला की उत्कृष्ट उपलब्धि है ।
यहां यह बता देना आवश्यक है कि ओड़िशा के बाद के मंदिरों में, जिनमें लिंगराज भी शामिल है, एक ही धुरी पर दो अतिरिक्त पूजा-स्थल जोड़े गए हैं – जगमोहन के सामने एक नटमंडप या नृत्य और संगीत का कक्ष और एक भोगमंडप, जो कि चढ़ाने के लिए एक विशाल कक्ष था । वास्तव में मंदिर एक संपूर्ण कलाकृति था जिसमें न केवल मूर्तियां व चित्र बल्कि संगीत, नृत्य और रंगमंचीय प्रदर्शन भी होते थे । वास्तव में यह कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया जो कि आधुनिक सामुदायिक केंद्रों की भांति था जो सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मिलन का स्थान हैं । पुरातन काल में इस कार्य का निर्वाह मंदिर करता था और वास्तव में समुदाय के नागरिक और धार्मिक जीवन का केंद्र था ।
भुवनेश्वर में बाद में बने मंदिरों में सन् 1278 में स्थापित अनंत वसुदेव मंदिर कई तरह से विशिष्ट है । मुख्य रूप से शैव स्थल पर वैष्णव आराधना को समर्पित यह एक मात्र मंदिर है जो कि एक अलंकृत चबूतरे पर खड़ा हुआ है । यह मंदिर लिंगराज की विनियोजित योजना और अलंकरण के अनुसार बना है लेकिन क्रमिक आरोहण में चार उपखंडों के ऊपर छतों का समूहीकरण यहां पर ज्यादा भव्य है । इसके अलावा गर्भगृह और जगमोहन की दीवारों पर राजाओं और उनकी पत्नियों के चित्र बने हैं ।
ओड़िशा की कलात्मक और स्थापत्य प्रतिभा की भव्यतम उपलब्धि कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण पूर्व गंग शासक नरसिम्ह वर्मन ने सन् 1250 ईसवी में करवाया था । इस विशाल और भव्य मंदिर की परिकल्पना एक विशाल रथ के रूप में की गई थी जिसके 12 जोड़ी सजावटी पहिये हैं और जिसे सात घोड़े खींच रहे हैं जो अपने पिछले पैरों पर खड़े हैं । इस विशाल मंदिर में मूलत: एक गर्भ-गृह है जिसके ऊपर एक वक्ररेखी शिखर है, एक जगमोहन और नृत्य कक्ष हैं जो कि समान धुरी पर बने हैं और तीन प्रवेशद्वार वाली एक विशाल अहाते की दीवार है । गर्भ-गृह और नृत्य कक्ष की छतें गिर चुकी हैं जबकि जगमोहन की छत अब भी है । गर्भ-गृह और जगमोहन एक साथ एक विशाल चबूतरे पर खड़े हैं जो कि हाथियों, अलंकरण आभूषणों के बीच बनी मूर्तियां जिनमें से कुछ अत्यंत कामुक हैं, की चित्रवल्लरी से अलंकृत है । जगमोहन की विशालकाय छत जिसपर समतल पंक्तियां तीन चरणों में विभक्त हैं, पर आकर्षक मानवाकार स्त्री आकृतियां, नर्तक, करताल बजाते लोग व अन्य, प्रत्येक चरण को अलंकृत कर रहे हैं । अपनी भव्यता और मूर्तिमय कौशल के लिए अद्वितीय, जगमोहन के ऊपर धूप और छांव का प्रभावकारी भेद है ।
मध्य प्रदेश में भिलसा से 40 मील दूर स्थित, उदयपुर, एक अन्य प्राचीन और विलक्षण स्थल है । सन् 1059 और 1080 ईसवी में उदयादित्य परमार द्वारा निर्मित नीलकंठ या उदयेश्वर मंदिर उत्कृष्ट और बेहतरीन रूप से संरक्षित है । यह मंदिर एक डयोढ़ी, पिरामिडी छत और आधार से शिखर तक जाती चार परिमित सपाट पट्टियों से अलंकृत है; मध्य के स्थान को पुन: आभूषणों से अंलकृत किया गया है जिसमें मुख्य शिखर की लघु आकृति को फिर से दोहराया गया है । संपूर्ण इमारत को विशेष सूक्ष्मता और कोमलता से उकेरा गया है जिसमें शिक्षर और मंडल दोनों ही पूर्ण रूप से संरक्षित हैं । शिखर पर एक अमलशिला या गुलदान रखा हुआ है ।
पट्टदकल के सबसे महत्त्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण 8वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ और इनपर पल्लव प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । लोकेश्वर के रूप में शिव को समर्पित भव्य वीरूपाक्ष मंदिर को 740 इसवी में विक्रमादित्य की रानी ने बनाया था । इसका निर्माण संभवत: कांचीपुरम से लाए गए कारीगरों ने किया था और यह कांचीपुरम के ही कैलाशनाथ की अनुकृति है ।
मुख्य पूजा स्थल मंडप से अलग है और इसमें एक प्रदक्षिणा पथ है । स्तंभों वाले मंडप की मज़बूत दीवारों पर पत्थर के छिद्रित झरोखे हैं । चौकोर शिखर में प्रत्येक मंजिल, जो कि काफी ऊपर उठी हुई हैं, को स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है । झरोखों पर चैत्य नमूनों का विस्तृत प्रयोग किया गया है और यहां पर अनेक तक्षित स्तंभ सरदल, पटिया और एकाश्म स्तंभ हैं । आरंभिक द्रविड़ मंदिर निर्माण पद्धतियों के अनुरूप इसका निर्माण बिना गारे के ध्यानपूर्वक जोड़े गए शिलाखंडों से किया गया है । भारत के भव्यतम मंदिरों में से एक पट्टदकल का यह एकमात्र प्राचीन मंदिर है जहां आज भी पूजा होती है ।
आइए अब हम दक्षिण भारत पर दृष्टि डालें जहां मंदिर वास्तुकला की द्रविण शैली का लगभग 8वीं शताब्दी से 13-14 शताब्दी ईसवी तक विकास हुआ । उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में हज़ारों मंदिर हैं क्योंकि उत्तर की भांति दक्षिण भारत को निरंतर विदेशी हमलों की मार नहीं झेलनी पड़ी । देश की स्थापत्य उपलब्धियों के पीछे हिंदुओं की अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति की सोच थी । मंदिर का निर्माण और रखरखाव सबके लिए पुण्य या धर्म का कार्य बन गया चाहे वह राजा हो, अभिजात वर्ग हो या आम आदमी । मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र बन गया, एक ऐसा केंद्र जिसके इर्द-गिर्द सारी गतिविधियां घूमती थीं । इसका प्रभाव केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था । मंदिर हर प्रकार की गतिविधि का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया था । राजा, अभिजात वर्ग और आम लोगों से भूमि अनुदान में पाकर मंदिर के पास बड़ी संख्या में भूसंपत्ति एकत्रित हो गई । मंदिर के निर्माण में अक्सर अनेक वर्ष लगते थे और इससे अनेक कलाकारों और अभियंताओं को रोज़गार मिलता था । पड़ोसी प्रांतों से उत्कृष्ट कामगारों को रोज़गार मिला और इसके निर्माण के दौरान उन्होंने प्रतिभावान मूर्तिकारों की एक पूरी पीढ़ी को प्रशिक्षित किया । दैनिक कार्यकलाप ने अनेक लोगों को निश्चित रूप से रोज़गार दिया जैसे कि पुजरी, संगीतज्ञ, नर्तकियां, शिक्षक, पुष्पविक्रेता, दर्जी इत्यादि । समय के साथ साधारण, आंडबर रहित मंदिर इमारतों का एक विशाल समूह बन गए जिसमें गौण मंदिर, नटमंडप और भोगमंडप अथवा नृत्य कक्ष या दान कक्ष शामिल थे । कवि मंडप, हलवाई और अन्य को मंदिर परिसर का हिस्सा बनने की अनुमति थी । दूसरे शब्दों में मंदिर ने नगर को अपने में समेट लिया या कि नगर ने मंदिर को अपने में । इन अतिरिक्त इमारतों में बढ़ोत्तरी के कारण मूल मंदिर परिसर में और अहाते जोड़े गए, एक के अंदर एक, चीनी डिब्बों की भांति ।
इस कारण वर्तमान दक्षिण भारतीय मंदिरों में एक के अंदर एक दीवारें और प्रांगण हैं । इस क्षेत्र की भीतरतम दीवार के अंदर एक दीवार और प्रांगण हैं । इस क्षेत्र की भीतरतम दीवार के अंदर मुख्य मंदिर है जिसका प्रवेशद्वार अन्य विशाल प्रवेशद्वारों की तुलना में कहीं छोटा और साधारण है । लेकिन अब वास्तुकारों, मूर्तिकारों और नक्काशी करने वालों की इसमें रूचि जागने लगी है । लगभग 1000 ईसवी में बना बृहदीश्वर मंदिर, भुवनेश्वर के राजरानी मंदिर का समकालीन है । एक भव्य और प्रतिष्ठित इमारत इस मंदिर का पिरामिडी शिखर निरंतर अवरोहात्मक मंजिलों से बना है जो कि ऊपर की ओर बढ़ते हुए सँकरा होता जाता है और इनका शीर्ष गुंबदाकार है । कई मायनों में यह मंदिर महाबलीपुरम् के तट पर बने मंदिरों की भांति है । लेकिन इसका गुंबदाकार शीर्ष ओडिशा के मंदिर के अम्लक से परिकल्पना और निष्पादन में भिन्न हैं । सबसे ऊँचा शिखर गर्भ-गृह के ऊपर बना है । संपूर्ण इमारत, अंदर और बाहर, सुंदर मूर्तियों और चित्रों से अलंकृत है । शिव को समर्पित बृहदीश्वर मंदिर 500 फ़ीट गुणा 200 फ़ीट के परिसर में खड़ा है । इसमें एक गर्भ-गृह, विशाल कक्ष, स्तंभों वाला बड़ा कक्ष और एक नटमंडप है जो सभी एक ही धुरी पर बने हुए हैं । 190 फीट ऊँचे पिरामिडी विमान में अवरोहात्मक क्रम में 13 मंडल हैं और इसकी परिकल्पना इस प्रकार की गई है कि दिन के किसी भी समय इसके शिखर की परछाई मंदिर के आधार के बाहर न पड़े ।
एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर एक उत्कृष्ट शैलोत्कीर्ण मंदिर परिसर है । इसमें और महाबलीपुरम् के विभिन्न रथों में अनेक समानताएं हैं । आठवीं शताब्दी ईसवी के मध्य में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के शासन काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ । एलोरा के मूर्तिकारों ने चट्टान के नीचे तीन खाइयां खोदीं और फिर ऊपर से लेकर नीचे तक पत्थर को तराशना आरंभ किया । हालांकि इसे एक मूर्तिमय मंदिर की भांति तराशा गया है, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर एक आयताकार परिसर के अंदर शैलोत्कीर्ण मंदिर है । मंदिर के विभिन्न भाग हैं- प्रवेश द्वार मंडप, विमान और मंडप तथा शिव के बैल, नंदी के लिए स्तंभों वाला एक मंदिर । मंदिर को अंदर तथा बाहर सुंदर, लालित्यपूर्ण और भव्य मूर्तियों द्वारा अलंकृत किया गया है जो कि शिव-पार्वती, सीता हरण और रावण के पर्वत हिलाने के प्रसंग पर आधारित हैं ।
गोपुरम एक आयताकार चतुष्कोण है जिसका आकार कभी-कभी चौकोर भी होता है । इसके बीच से एक मार्ग और उत्तर भारत से भिन्न यह प्रवेशद्वार पर स्थित है । तंजोर के बृहदीश्वर मंदिर में भी शिखर जैसा ढांचा गर्भ-गृह के ऊपर था । कई मानों में गोपुरम बौद्ध प्रवेशद्वार की उत्पत्ति हो सकता था जैसा कि हमने सांची और भरहुत इत्यादि में देखा है । इसके ऊपर एक बेलनाकार मेहराबी छत है जिसके ऊपर से अनेक शीर्ष दिखते हैं जो कि हमें पुन: इमारती लकड़ी से बनी लंबी झोंपड़ी की ढोलाकार छत की याद दिलाती है । जैसा कि पहले बताया गया है, ये गोपुरम विशाल थे जिनमें किसी-किसी की 9 से लेकर 11 तक मंजिलें होती थीं । गोपुरम में मूर्तिकार को अपने शिल्प का अभ्यास करने का सर्वोत्तम अवसर मिला और इनमें देश के सर्वोत्तम शिल्प पाए जा सकते हैं । चिदंबरम के गोपुरम में भरतनाटयम की नृत्य मुद्राओं को शिल्प शृंखला के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है । रात के समय गोपुरम के शिखर की प्रत्येक मंजिल को प्रज्ज्वलित किया जाता था और ये रात के मुसाफिरों के लिए प्रकाशगृह या संकेत-दीप का काम करती थीं । नियमानुसार सबसे ऊँचे गोपुरम का शिखर नवीनतम था, प्रारंभिक सबसे कम ऊँचा जैसा कि मदुरै के मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम में दिखाई देता है । आगंतुक इन मीनारों पर चढ़कर पास से नक्काशी का रसास्वादन कर सकते हैं । इस काल के दक्षिण भारतीय मंदिर अपने ढांचे, मंडप और गोपुरम के विशाल आकार के लिए जाने जाते हैं । इसके अतिरिक्त उत्तर विजयनगर काल और 16वीं शताब्दी ईसवी में नायकों के शासनकाल के दौरान सौ स्तंभ सरीखे विस्तृत मंडपों का भी निर्माण किया गया । प्राचनी काल की तुलना में यहां मंदिरों के विकास में अंतर था । स्तंभों वाले ये कक्ष ज्यादा अलंकृत होते जा रहे हैं जिनमें स्तंभों पर दान करने वाले जोड़े, राजा, रानी, विभिन्न आकार और माप के कल्पित पशु दर्शाए गए हैं । इनके और स्तंभों तथा भीतरी छत के ऊपर बनाए गए चित्रों में अनेक रंगों का प्रयोग किया गया है ।
कुछ मंदिरों में जलाशयों के इर्द-गिर्द सुरुचिपूर्ण स्तंभों वाले विशाल कक्ष हैं जो कि कार्यात्मक और वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट इमारतें हैं । मैसूर के होयसल शासकों ने 12वीं-13वीं शताब्दी में सोमनाथपुर, बेलूर और हैलेबिड में मंदिरों का निर्माण कराया । सोमनाथपुर का प्रसिद्ध केशव मंदिर और हैलेबिड और बेलूर के होयसल मंदिर अलंकृत और सज़ावटी तत्त्वों की संपदा है । ये अपने उकेरे गए आलों और बारीकी से उत्कीर्ण किए गए वनस्पति और पुष्पों के लिए प्रसिद्ध हैं । योजना में तारे के आकार के विमान में बहिर्गत और पुनर्प्रवेशी कोण हैं जिनपर ढांचे, गुणन और अत्यधिक अलंकरण किया गया है । कोई भी स्थान नक्काशी रहित नहीं है । पशु व अन्य वनवासियों को निचले तीन या चार ढांचों में दिखाया गया है जिनके बीच पुष्प और लताएं भी हैं । इन सबसे ऊपर, मानवाकृति से भी विशाल देवी-देवताओं की विशाल मूर्तियां हैं जो अत्यधिक अलंकरणों और मूल्यवान आभूषणों से ढकी हुई हैं ।
मध्य प्रदेश में पन्ना से 25 मील दूर उत्तर में और छतरपुर से 27 मील दूर खजुराहो, चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट मंदिरों के कारण एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । खजुराहो के मंदिरों की योजना स्वस्तिकाकार है जिसमें पूर्व से पश्चिम तक लंबी धुरी है । पन्ना की खदानों से मिले मटमैले बलुआ पत्थरों से निर्मित इन मंदिरों की संरचना मृदु और रंग अत्यंत सुहावना है । मंदिरों को अक्सर ऊँचे टीलों पर बनाया गया है । लगभग सभी मंदिरों में एक भीतरी पूजा स्थल, मंडप और प्रवेश मंडप था । खजुराहो के मंदिर में एक प्रदक्षिणा पथ भी था । खजुराहो के कुछ मंदिर पांच पूजा स्थलों का एक समूह हैं जिसमें से मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर चार मंदिर हैं । वास्तुकला में इस प्रकार के मंदिरों को पंचायतन कहा जाता है यानि कि एक मंदिर जिसमें एक केंद्रीय पूजा-स्थल के इर्द-गिर्द चार अन्य पूजा स्थल हैं ।
कुछ प्रसिद्ध मंदिर जो कि कला और वास्तुकला की दृष्टि से अध्ययन के योग्य हैं- कंदरीय मंदिर, महादेव मंदिर, देवी जगदंबा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण या चतुर्भुज मंदिर, वराह मंदिर और चौंसठ योगिनी मंदिर ।
इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था । खजुराहो का दक्षिण पूर्व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है । पार्श्वनाथ मंदिर सबसे प्रमुख है जबकि घंटई मंदिर का नाम इसके स्तंभों पर बनी घंटी और कडि़यों के कारण पड़ा ।
पाल और सेन शासक
आठवीं से बारहवीं शताब्दी के बची भारत का उत्तरी भाग गहन कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा । पूर्वी-दक्षिण एशिया के विशाल हिस्सों पर शासन करने वाले पाल वंश के शासन काल के दौरान बौद्ध और हिंदू धर्म के अनेक केन्द्र उन्नत हुए ।
पाल वंश ने 750 ईसवी के लगभग सत्ता संभाली । पाल कला शैली सर्वप्रथम दक्षिण बिहार के मगध क्षेत्र में फली-फूली जो बौद्ध धर्म की जन्मस्थली था । इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि पाल काल के प्रारंभिक अवशेष बौद्ध हैं । पाल-सेन काल के दौरान गहन धार्मिक गतिविधि के चलते अनेक धार्मिक इमारतों का निर्माण या जीर्णोद्धार हुआ । इनमें से अधिकांश इमारतें अब नष्ट हो चुकी हैं जिसके कारण इस काल की वास्तुकला अब लुप्त हो गई है । इस कारण वास्तुकला के विकास के क्रमबद्ध पर्यवलोकन को पुनर्निर्मित करना और कठिन हो गया है । किसी भी इमारत के मौजूद न होने के बावज़ूद भी इस काल के शिल्पकला के विशाल भंडार और चित्र अभी तक मौजूद हैं ।
पाल काल के दौरान विगत कालों में स्थापित अनेक मठ और धार्मिक स्थलों की महत्ता बढ़ी । बंगाल (अब बांग्लादेश) में स्थित पहाड़पुर (प्राचीन सोमपुरा) का विशाल स्वस्तिकाकार स्तूप उत्तर से दक्षिण तक 100 मीटर से भी अधिक लंबा है । इसका निर्माण आठवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध या नवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ था । अहाते की दीवार में 177 अलग-अलग कक्ष हैं जो मंदिर का हिस्सा थे । हालांकि पाल काल की कला के पहले लगभग 200 वर्षों में बौद्ध कला का वर्चस्व था, लेकिन यहां से प्राप्त कुछ हिंदू अवशेषों से स्पष्ट है कि पाल कला के अंतिम दो सौ वर्षों में इनका वर्चस्व था ।
हालांकि अवशेष खंडित अवस्था में हैं, लेकिन उन्हें देखकर पता चलता है कि उनमें और बंगाली वास्तुकला शैली, विशेषकर अन्य उत्तरी शैलियों, खासकर ओडि़या शैली में समानताएं हैं । पाल-सेन काल के बाद की बंगाल की कला (विशेषकर 16वीं शताब्दी से) में बढ़ता हुआ इस्लामिक प्रभाव नज़र आता है । अत: आठवीं से 12वीं शताब्दी तक हिंदू कलात्मक विकास को समझने के लिए मौजूदा मूर्तियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए ।