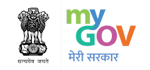संगीत वाद्ययंत्र
भारत विश्व में, सबसे ज्यादा प्राचीन और विकसित संगीत तंत्रों में से एक का उतराधिकारी है । हमें इस परम्परा की निरंतरता का ज्ञान संगीत के ग्रंथों और प्राचीन काल से लेकर आज तक की मूर्तिकला और चित्रकला में संगीत वाद्यों के अनेक दृष्टांत उदाहरणों से मिलता है ।
हमें संगीत-सम्बंधी गतिविधि का प्राचीनतम प्रमाण मध्यप्रदेश के अनके भागों और भीमबटेका की गुफाओं में बने भित्तिचित्रों से प्राप्त होता है, जहां लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव निवास करता था । इसके काफी समय बाद, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से भी नृत्य तथा संगीत गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं ।
संगीत वाद्य, संगीत का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं । इनका अध्ययन संगीत के उदभव की जानकारी देने में सहायक होता है और वाद्य जिस जनसमूह से सम्बंधित होते हैं, उसकी संस्कृति के कई पहलुओं का भी वर्णन करते हैं । उदाहरण के लिए गज बनाने के लिए बाल, ढोल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी या चिकनी मिट्टी या फिर वाद्यों में प्रयुक्त की जाने वाली जानवरों की खाल यह सभी हमें उस प्रदेश विशेष की वनस्पति तथा पशु-वर्ग की विषय में बताते हैं ।
दूसरी से छठी शताब्दी ईसवी सन् के संगम साहित्य में वाद्य के लिए तमिल शब्द ‘कारूवी’ का प्रयोग मिलता है । इसका शाब्दिक अर्थ औजार है, जिसे संगीत में वाद्य के अर्थ में लिया गया है ।
बहुत प्राचीन वाद्य मनुष्य के शरीर के विस्तार के रूप में देखे जा सकते हैं और जहां तक कि हमें आज छड़ी ओर लोलक मिलते हैं । सूखे फल के बीजों के झुनझुने, औरांव के कनियानी ढांडा या सूखे सरस फल या कमर पर बंधी हुई सीपियों को ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आज भी प्रयोग में लाया जाता है ।
हाथ का हस्तवीणा के रूप में उल्लेख किया गया है, जहां हाथों व उंगलियों को वैदिक गान की स्वरलिपि पद्धति को प्रदशर्ति करने तथा ध्वनि का मुद्रा-हस्तमुद्रा के साथ समन्वय करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।
200 ईसा पूर्व से 200 ईसवीं सन् के समय में भरतमुनि द्वारा संकलित नाटयशास्त्र में संगीत वाद्यों को ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है :
1. तत् वाद्य अथवा तार वाद्य – तार वाद्य
2. सुषिर वाद्य अथवा वायु वाद्य – हवा के वाद्य
3. अवनद्व वाद्य और चमड़े के वाद्य – ताल वाद्य
4. घन वाद्य या आघात वाद्य – ठोस वाद्य, जिन्हें समस्वर स्तर में
करने की आवश्यकता नहीं होती ।
तत् वाद्य – तारदार वाद्य
तत् वाद्य, वाद्यों का एक ऐसा वर्ग है, जिनमें तार अथवा तन्त्री के कम्पन से ध्वनि उत्पन्न होती है । यह कम्पन तार पर उंगली छेड़ने या फिर तार पर गज चलाने से उत्पन्न होती हैं । कम्पित होने वाले तार की लम्बाई तथा उसको कसे जाने की क्षमता स्वर की ऊंचाई (स्वरमान) निश्चित करती है और कुछ हद तक ध्वनि की अवधि भी सुनिश्चित करती है । तत् वाद्यों को मोटे पर दो भागों में विभाजित किया गया है- तत् वाद्य और वितत् वाद्य । आगे इन्हें सारिका (पर्दा) युक्त और सारिका विहीन (पर्दाहीन) वाद्यों के रूप में पुन: विभाजित किया जाता है ।
हमारे देश में तत् वाद्यों का प्राचीनतम प्रमाण धनुष के आकार की बीन या वीणा है । इसमें रेशे या फिर पशु की अंतडि़यों से बनी भिन्न-भिन्न प्रकार की समानांतर तारें होती थीं । इसमें प्रत्येक स्वर के लिए एक तार होती थी, जिन्हें या तो उंगलियों से छेड़ कर या फिर कोना नामक मिज़राब से बजाया जाता था । संगीत के ग्रंथों में तत् (तारयुक्त वाद्यों) वाद्यों के लिए सामान्य रूप से ‘वीणा’ शब्द का प्रयोग किया जाता था और हमें एक-तंत्री, संत-तंत्री वीणा आदि वाद्यों की जानकारी मिलती है । चित्रा में सात तारें होती हैं और विपंची में नौ । चित्रा को उंगलियों द्वारा बजाया जाता था और विपंची का मिज़राब से ।
प्राचीन समय की बहुत-सी-मूर्तियों और भित्तिचित्रों से इनका उल्लेख प्राप्त होता है । जैसे भारूत और सांची स्तूप, अमरावती के नक्काशीदार स्तम्भ आदि । दूसरी शताब्दी ईसवीं सन् के प्राचीन तमिल ग्रंथों में याड़ का उल्लेख प्राप्त होता है । धार्मिक अवसरों और समारोहों में ऐसे वाद्यों को बजाना महत्वपूर्ण रहा है । जब पुजारी ओर प्रस्तुतकर्ता गाते थे तो उनकी पत्नी वाद्यों को बजाती थीं ।
डेलसिमर प्रकार के वाद्य तारयुक्त वाद्यों का एक अन्य वर्ग है । इसमें एक लकड़ी के बक्से पर तार खींच कर रखे जाते हैं । इसका सबसे अच्छा उदाहरण है- सौ तारों वाली वीणा अर्थात् सत-तंत्री वीणा । इस वर्ग का निकटतम सहयोगी वाद्य है- संतूर । यह आज भी कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में बजाया जाता है ।
बाद में तारयुक्त वाद्यों के वर्ग में डांड़ युक्त वाद्यों के भी एक वर्ग का विकास हुआ । यह राग-संगीत से जुड़े, प्रचलित वाद्यों के लिए उपयुक्त था । चाहे वह पर्दे वाले वाद्य हों अथवा पर्दा विहीन वाद्य हों, उंगली से तार छेड़ कर बजाए जाने वाले वाद्य हों, अथवा गज से बजाए जाने वाले- सभी इसी वर्ग में आते हैं । इन वाद्यों का सबसे बड़ा महत्व है- स्वर की उत्पत्ति की समृद्धता और स्वर की नरंतरता को बताए रखना । डांड युक्त वाद्यों में सभी आवश्यक स्वर एक ही तार पर, तार की लम्बाई को उंगली द्वारा या धातु अथवा लकड़ी के किसी टुकड़े से दबा कर, परिवर्तित करके उत्पन्न किए जा सकते हैं । स्वरों के स्वरमान में परिवर्तन के लिए कंपायमान तार की लम्बाई का बढ़ना या घटना महत्वपूर्ण होता है ।
गज वाले तार वाद्य आमतौर पर गायन के साथ संगत के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तथा गीतानुगा के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है । इन्हें दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है । पहले वर्ग में सारंगी के समान डांड़ को सीधे ऊपर की ओर रखा जाता है और दूसरे वर्ग में तुम्बे की कंधे की ओर रखा जाता है तथा ‘डंडी’ या डांड़ को वादक की बांह के पार रखा जाता है । ठीक उसी प्रकार जैसे- रावण हस्तवीणा, बनाम तथा वायलिन में ।
कमैचा
कमैचा पश्चित राजस्थान के मगनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजायी जाने वाली वीणा है । यह संपूर्ण वाद्य लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना होता है, गोलाकार लकड़ी का हिस्सा गर्दन तथा डांड का रूप लेता है; अनुनादक (तुंबस) चमड़े से मढ़ा होता है और ऊपरी भाग लकड़ी से ढका होता है । इसमें चार मुख्य तार होते हैं और कई सहायक तार होते हैं, जो पतले ब्रिज (घुड़च) से होकर गुजरते हैं ।
कमैचा वाद्य उप महाद्वीप को पश्चिम एशिया और अफ्रीका से जोड़ता है और इसे कुछ विद्वान रावन हत्ता अथवा रावण हस्त वीणा के अपवाद स्वरूप प्राचीनतम वाद्य के रूप में स्वीकार करते है ।
लम्बवत् गजयुक्त वाद्यों के प्रकार सामान्यत: देश के उत्तरी भागों में पाए जाते हैं । इनमें आगे फिर से दो प्रकार होते हैं- सारिका (पर्दा) युक्त और सारिकाविहीन (पर्दाविहीन) ।
(क) तारदार वाद्य के विविध हिस्से
अनुनादक (तुम्बा)-अधिकतर तारदार वाद्यों का तुम्बा या तो लकड़ी काबना होता है या फिर विशेष रूप से उगाए गए कहू का ।
इस तुम्बे के ऊपर एक लकड़ी की पट्ट होती है, जिसे तबली कहते हैं ।
अनुनादक (तुम्बा), उंगली रखने की पट्टिका-डांड से जुड़ा होता है, जिसके ऊपरी अंतिम सिरे पर खूंटियां लगी होती हैं । इनको वाद्य में उपयुक्त स्वर मिलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।
तबली के ऊपर हाथीदांत से बना ब्रिज (घुड़च) होता है । मुख्य तार इस ब्रिज या घुड़च के ऊपर से होकर जाते हैं । कुछ वाद्यों में इन मुख्य तारों के नीचे कुछ अन्य तार होते हैं, जिन्हें तरब कहा जाता है । जब इन तारों को छेड़ा जाता है तो यह गूंज पैदा करते हैं ।
कुछ वाद्यों में डांड पर धातु के पर्दे जुड़े होते हैं, जो स्थाई रूप से लगे होते हैं या फिर ऊपर-नीचे सरकाए जा सकते हैं । कुछ तार वाद्यों को उंगलियों से छेड़ कर या फिर कोना नामक छोटी मिज़राब की सहायता से बजाया जाता है । जबकि अन्य तार वाद्यों को गज की सहायता से बजाया जाता है । (देखें आरेख ए)
(ख) स्वरों के स्थान
प्रस्तुत रेखाचित्र-स्वरों के स्थान तथा 36 इंच की तार पर सा रे म ग प ध नि सा स्वरों को दिखाता है । चित्र में प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या भी दिखाई गई है । (देखें आरेख बी)
सुषिर वाद्य
सुषिर वाद्यों में एक खोखली नलिका में हवा भर कर (अर्थात फूंक मार कर) ध्वनि उत्पन्न की जाती है । हवा के मार्ग को नियंत्रित करके स्वर की ऊंचाई सुनिश्चित की जाती है और वाद्य में बने छेदों को उंगलियों की सहायता से खोलकर और बाद करके क्रमश: राग को बजाया जाता है । इस सभी वाद्यों में सबसे सर (साधारण) वाद्य है-बांसुरी । आम तौर पर बांसुरियां बांस अथवा लकड़ी से बनी होती हैं और भारतीय संगीतकार संगीतात्मक तथा स्वर-सम्बंधी विशेषताओं के कारण लकड़ी तथा बांस की बांसुरी को पसंद करते हैं । हालांकि यहां लाल चंदन की लकड़ी, काली लकड़ी, बेंत, हाथी दांत, पीतल, कांसे, चांदी और सोने की बनी बांसुरियों के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं ।
बांस से बनी बांसुरियों का व्यास साधारणत: करीब 1.9 से.मी. होता है पर चौड़े व्यास वाली बांसुरियां भी आमतौर पर उपयोग में लाई जाती हैं । 13वीं शताब्दी में शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत सम्बंधी ग्रंथ ‘संगीत रत्नाकर’ में हमें 18 प्रकार की बांसुरियों का उल्लेख मिलता है । बांसुरी के यह विविध प्रकार फूंक मारने वाले छेद और पहली उंगली रखने वाले छेद के बची की दूरी पर आधारित हैं (आरेख देखें)
सिन्धु सभ्यता की खुदाई में मुत्तिका शिल्प (मिट्टी) की बनी पक्षी के आकार की सीटियां और मुहरें प्राप्त हुई हैं, जो हवा और ताल वाद्यों को प्रदर्शित करती हैं । बांस, लकड़ी तथा पशु की खाल आदि से बनाए गए संगीत वाद्य कितने भी समय तक रखे रहें, वे नष्ट हो जाते हैं । यही कारण है कि लकड़ी या बांस की बनी बांसुरियां समय के आघात को नहीं सह पाईं । इसी कारणवश हमें पिछली सभ्यताओं की किसी खुदाई में ये वाद्य प्राप्त नहीं होते ।
यहां वेदों में ‘वेनू’ नामक वाद्य का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे राजाओं का गुणगान तथा मंत्रोच्चारण में संगत करने के लिए बजाया जाता था । वेदों में ‘नांदी’ नामक बांसुरी के एक प्रकार का भी उल्लेख प्राप्त होता है । बांसुरी के विविध नाम हैं, जैसे उत्तर भारत में वेणु, वामसी, बांसुरी, मुरली आदि और दक्षिण भारत में पिल्लनकरोवी और कोलालू ।
ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर मोटे तौर पर सुषिर अथवा वायु वाद्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है-
– बांसुरियां और
– कम्पिका युक्त वाद्य
बांसुरी
इकहरी बांसुरी अथवा दोहरी बांसुरियां केवल एक खोखली नलिका के साथ, स्वर की ऊँचाई को नियंत्रित करने के लिए अंगुली रखने के छिद्रों सहित होती हैं । ऐसी बांसुरियां देश के बहुत से भागों में प्रचलित हैं । लम्बी, सपाट, बड़े व्यास वाली बांसुरियों को निचले (मंद्र) सप्तक के आलाप जैसे धीमी गति के स्वर-समूहों को बजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । छोटी और कम लम्बाई वाली बांसुरियों को, जिन्हें कभी-कभी लम्बवत् (उर्ध्वाधर) पकड़ा जाता है, द्रुत गति के स्वर-समूह अर्थात् तान तथा ध्वनि के ऊंचे स्वरमान को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है । दोहरी बांसुरियां अक्सर आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्र के संगीतकारों द्वारा बजाई जाती हैं और ये मंच-प्रदर्शन में बहुत कम दिखाई देती हैं । ये बांसुरियां चोंचदार बांसुरियों से मिलती-जुलती होती हैं, जिनके एक सिरे पर संकरा छिद्र होता है । हमें इस प्रकार के वाद्यों का उल्लेख प्रथम शताब्दी के सांची के स्तूप के शिल्प में प्राप्त होता है, जिसमें एक संगीतकार को दोहरी बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया हे ।
कम्पिका वाद्य
कम्पिका या सरकंडा युक्त वाद्य जैसे शहनाई, नादस्वरम् आदि वाद्यों में वाद्य की खोखली नलिका के भीतर एक अथवा दो कम्पिका को डाला जाता है, जो हवा के भर जाने पर कम्पित होती हैं । इस प्रकार के वाद्यों में कम्पिकाओं को नलिका के भीतर डालने से पहले एक साथ, एक अंतराल में बांधा जाता है । नलिका शंकु के आकार की होती है । यह हवा भरने वाले सिरे की तरफ से संकरी होती है और धीरे-धीरे दूसरे सिरे पर खुली होती जाती है तथा एक धातु की घंटी का आकार ले लेती है, ताकि ध्वनि की प्रबलता को बढ़ाया जा सके । वाद्य के मुख से एक अतिरिक्त कम्पिकाओं का समूह और कम्पिकाओं को साफ करने तथा व्यवस्थित रखने के लिए हाथीदांत अथवा चांदी की एक सुई लटकाई जाती है ।
शहनाई
शहनाई एक कम्पिका युक्त बांध है । इसमें नलिका के ऊपर सात छिद्र होते हैं । इन छिद्रों को अंगुलियों से बंद करने और खोलने पर राग बजाया जा सकता है । इस वाद्य को ‘मंगल वाद्य’ के नाम से जाना जाता है और अक्सर इसे उत्तर भारत में विवाह, मंदिर उत्सवों आदि के मंगलवार अवसर पर बजाया जाता है । ऐसा माना जाता है कि शहनाई भारत में पश्चिम एंशिया से आई । कुछ अन्य विद्वान भी हैं, जो यह मानते हैं कि यह वाद्य चीन से आया है । इस समय यह वाद्य कार्यक्रमों में बजाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य है । वाद्य ही आवाज़ सुरीली होती है और यह राग संगीत को बजाने के लिए उपयुक्त है । इस शताब्दी के सन् पचास के दशक के पूर्व भाग में इस वाद्य को प्रसिद्ध बनाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है । आज के जाने-माने शहनाई वादकों में पंडित अनंत लाल और पंडित दया शंकर का नाम प्रमुख है ।
अवनद्ध वाद्य
वाद्यों के वर्ग, अवनद्ध वाद्यों (ताल वाद्य) में पशु की खाल पर आघात करके ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है, जो मिट्टी, धातु के बर्तन या फिर लकड़ी के ढोल या ढांचे के ऊपर खींच कर लगायी जाती है । हमें ऐसे वाद्यों के प्राचीनतम उल्लेख वेदों में मिलते हैं । वेदों में भूमि दुंदुभि का उल्लेख है । यह भूमि पर खुदा हुआ एक खोखला गढ़ा होता था, जिसे बैल या भैंस की खाल से खींच कर ढका जाता था । इस गढ़े के खाल ढके हिस्से पर आघात करने के लिए पशु की पूंछ को प्रयोग में लाया जाता था और इस प्रकार से ध्वनि की उत्पत्ति की जाती थी ।
ढोलों को उनके आकार, ढांचे तथा बजाने के लिए उनको रखे जाने के ढंग व स्थिति के आधार पर विविध वर्गों में बांटा जा सकता है । ढोलों को मुख्यत: अर्ध्वक, अंकया, आलिंग्य और डमय (ढालों का परिवार) इन चार वर्गों में बांटा जाता है । (आरेख देखें)
उर्ध्वक
उर्ध्वक ढालों को वादक के समक्ष लम्बवत् रखा जाता है और इन पर डंडियों या फिर उंगलियों से आघात करने पर ध्वनिं उत्पन्न होती है । इनमें मुख्य हैं-तबले की जोड़ी और चेंडा ।
तबला
तबले की जोड़ी दो लम्बवत् ऊर्ध्वक ढोलों का एक समूह है । इसके दायें हिस्से को तबला कहा जाता है और बांये हिस्से को बांया अथवा ‘डग्गा’ कहते हैं । तबला लकड़ी का बना होता है । इस लकड़ी के ऊपरी हिस्से को पशु की खाल से ढका जाता है और चमड़े की पट्टियों की सहायता से जोड़ा जाता है । चर्म पट्टियों तथा लकड़ी के ढांचे के बीच आयताकार (चौकोर) लकड़ी के खाल के हिस्से के बीच में स्याही को मिश्रण लगाया जाता है । तबले को हथौड़ी से ऊपरी हिस्से के किनारों को ठोंक कर उपयुक्त स्वर को मिलाया जा सकता है । बांया हिस्सा मिट्टी अथवा धातु का बना होता है । इसका ऊपरी हिस्सा पशु की खाल से ढंका जाता है और उस पर भी स्याही का मिश्रण लगाया जाता है । कुछ संगीतकार इस हिस्से को सही स्वर में नहीं मिलाते ।
तबले की जोड़ी को हिन्दुस्तानी संगीत के कंठ तथा वाद्य-संगीत और उत्तर भारत की कई नृत्य शैलियों के साथ संगत प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । तबले पर हिन्दुस्तानी संगीत के कठिन ताल भी बहुत प्रवीणता के साथ बजाए जाते हैं । वर्तमान समय के कुछ प्रमुख तबला वादक हैं-उस्ताद अल्ला रक्खा खां और उनके सुपुत्र ज़ाकिर हुसैन, शफात अहमद और सामता प्रसाद ।
तबला
तबले की जोड़ी दो लम्बवत् ऊर्ध्वक ढोलों का एक समूह है । इसके दायें हिस्से को तबला कहा जाता है और बांये हिस्से को बांया अथवा ‘डग्गा’ कहते हैं । तबला लकड़ी का बना होता है । इस लकड़ी के ऊपरी हिस्से को पशु की खाल से ढका जाता है और चमड़े की पट्टियों की सहायता से जोड़ा जाता है । चर्म पट्टियों तथा लकड़ी के ढांचे के बीच आयताकार (चौकोर) लकड़ी के खाल के हिस्से के बीच में स्याही को मिश्रण लगाया जाता है । तबले को हथौड़ी से ऊपरी हिस्से के किनारों को ठोंक कर उपयुक्त स्वर को मिलाया जा सकता है । बांया हिस्सा मिट्टी अथवा धातु का बना होता है । इसका ऊपरी हिस्सा पशु की खाल से ढंका जाता है और उस पर भी स्याही का मिश्रण लगाया जाता है । कुछ संगीतकार इस हिस्से को सही स्वर में नहीं मिलाते ।
तबले की जोड़ी को हिन्दुस्तानी संगीत के कंठ तथा वाद्य-संगीत और उत्तर भारत की कई नृत्य शैलियों के साथ संगत प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । तबले पर हिन्दुस्तानी संगीत के कठिन ताल भी बहुत प्रवीणता के साथ बजाए जाते हैं । वर्तमान समय के कुछ प्रमुख तबला वादक हैं-उस्ताद अल्ला रक्खा खां और उनके सुपुत्र ज़ाकिर हुसैन, शफात अहमद और सामता प्रसाद ।
आलिंग्य
तीसरा वर्ग आलिंग्य ढोल हैं । इन ढोलों में पशु की खाल को लकड़ी के एक गोल खांचे पर लगा दिया जाता है और गले या इसे एक हाथ से शरीर के निकट करके पकड़ा जाता है, जबकि दूसरे हाथ को ताल देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । इस वर्ग में डफ, डफली आदि आते हैं, जो बहुत प्रचलित वाद्य है ।
डमरू
डमरू ढोलों का एक अन्य प्रमुख वर्ग है । इस वर्ग में हिमाचल प्रदेश के छोटे ‘हुडुका’ से लेकर दक्षिणी प्रदेश का विशाल वाद्य ‘तिमिल’ तक आते हैं । पहले वाद्य को हाथ से आघात देकर बजाया जाता है, जबकि दूसरे को कंधे से लटका कर डंडियों और उंगलियों से बजाया जाता है । इस प्रकार के वाद्यों को रेतघड़ी वर्ग के ढोलों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका आकार रेतघड़ी से मिलता-जुलता प्रतीत होता है ।
घन वाद्य
मनुष्य द्वारा अविष्कृत सबसे प्राचीन वाद्यों को घन वाद्य कहा जाता है । एक बार जब यह वाद्य बन जाते हैं तो फिर इन्हें बजाने के समय कभी भी विशेष सुर में मिलाने की आवश्यकता नहीं होती । प्राचीन काल में यह वाद्य मानव शरीर के विस्तार जैसे डंडियों, तालों तथा छडि़यों आदि के रूप में सामने आए और ये दैनिक जीवन में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, जैसे पात्र (बर्तन), कड़ाही, झांझ, तालम् आदि के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए थे । मूलत: यह वस्तुएं लय प्रदान करती है और लोक तथा आदिवासी अंचल के संगीत तथा नृत्य के साथ संगत प्रदान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं ।
झांझ वादक, कोणार्क, उड़ीसा
उड़ीसा के कोर्णाक स्थित सूर्य मंदिर में हम एक 8 फीट ऊंचा शिल्प देख सकते हैं, जिसमें एक स्त्री को झांझ बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है ।