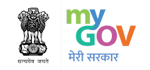मूर्तिकला के मध्यकालीन पीठ
पुणे जिले में कार्ले में भव्य प्रार्थना भवन या चैत्य लगभग सौ वर्ष पश्चात खोद कर निकाली गई एक गुफा है । इसकी खुदाई भी एक जीवित चट्टान से की गई है और यह अपनी ऊँची तथा उत्थापित छाप के लिए अद्वितीय है । इसका आकार वास्तव में विस्मयकारी है (124’ X 46-½’ X 45’) । इसके सुअनुपाती विशाल तथा भारी स्तम्भ हैं जो अपने आप में अत्यधिक मौलिकता की पूंजी को संजोए हुए हैं । इसकी छत मेहराबदार है जिसमें लकड़ी की वास्तविक कडि़यों का प्रयोग किया गया है, एक कमानी जो कि लकड़ी के ढांचे की नकल है । ये स्त़म्भ सुदृढ एवं भारी हैं, तक्षित बड़े अक्षरों द्वारा आच्छादित हैं । काफी दूरी पर एक स्तूप है जिसके शीर्ष पर लकड़ी की एक छतरी है और आश्चर्यजनक बात यह है कि मूल लकड़ी को अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंची है ।
अब मूर्तिकला का झुकाव शास्त्रीय गरिमा, सादगी और सौम्यता के स्थान पर अलंकरण, कला की अत्यधिक अलंकृत कृतियों, अर्द्ध मानव, अर्द्ध दैत्य आदि जैसे अनोखे तथा असामान्य जीवों की ओर अधिकाधिक है ।
कला शैली के इस नए रूप की विशेषता कुशलता और अभिक्षमता में नहीं बल्कि मुद्रा की शास्त्रीय कला की भिन्नता में निहित है । प्रारम्भिक शास्त्रीय काल के कलाकारों की ही भांति, सौन्दर्य और आदर्शीकरण अभी भी कलाकार को उत्साहित करते हैं, लेकिन अब अलंकरण से लगाव, सजावटी ब्यौरे शास्त्रीय सादगी पर हावी हो गए हैं । अब अधिक जटिलता, अलंकरण और समृद्वि है । एक त्रुटिपूर्ण मत यह है कि भारतीय कलाकार, प्रतिमाओं में भारतीय देवकुल के देवी-देवताओं को किस प्रकार से दिखलाना है, को विनिर्दिष्ट करने वाले शिल्पशास्त्रों में निर्धारित नियमों के कड़े अनुसरक थे । भारतीय मूर्तिकला की विविधता और विशिष्टता पर एक दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे-जैसे शैलियों का विकास हुआ मूर्तिकार प्राय: निर्धारित विषयों और नियमों से भटक गए तथा उन्हें मानव एवं यहां तक कि देव व देवियों के शरीर से विचलन और स्वतंत्रता लेने में आनंद आने लगा । हमारे द्वारा किसी तय देवता, यथा बुद्ध की प्रतिमा, की किन्हीं दो प्रतिमाओं के बीच तुलना करने पर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाएगा । मूर्तिकार ने पर्याप्त दक्षता, परिपक्वता और कुशलता ग्रहण कर ली है तो वह अपनी कलाकृति में कुछ विशिष्टता का समावेश कर सकता है, अपने युग में अपनी पसन्द और नापसन्द की अपनी अभिरुचियों की एक छाप छोड़ सकता है । यह परिपक्वता, जीवन एवं गतिशीलता का एक संकेत है।
युगों के दौरान शिल्पशास्त्र विषयों में निर्धारित नियमों के संबंध में कड़ाई से एकरूपता, पटुता और अनुरूपता हमारे देश में इस महान कला की अवनति में वृद्धि का एक संकेत होगा । यदि कला को उन्नति करनी है तो इसे अलग-अलग समय, प्रवृत्ति, पसन्द की परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना होगा और चूंकि समकालिक समाज को उसकी अपनी अलग-अलग पसन्द के साथ प्रतिबिम्बित करने का दायित्व अच्छी कला पर है, अत: शैली को भी बदलना होगा । भारतीय मूर्तिकला की भव्य कला और संग्रहालय में युगों की मूर्तियों पर एक दृष्टि डालने से आपको एक युग से अन्य युग तक इस जिज्ञासु मन को संतोष मिलेगा । इस युग के नए कलाकार की सर्वाधिक असाधारण उपलब्धि को एक ओर तो उड़ते हुए भगवान की आकृतियों में और शास्त्रीय अवधि की तुलना में अधिक स्वतंत्र संचलन में स्वप्निल तथा चलायमान गुणवत्ता का योगदान करना था तो वहीं दूसरी ओर रूप के लालित्य एवं छरहरेपन में वृद्धि करने के प्रति एक रुझान है ।
महिला में एक नया सौन्दर्य है । नितम्ब अधिक छरहरे हैं, कमर अधिक सुनम्य है, टांगें लम्बी हैं । चेहरा अभी भी रूढि के अनुसार ही है और वक्षस्थल परिपूर्ण तथा सुदृढ़ है । महिला अब एक देवी मां नहीं रह गई है बल्कि एक दिव्य सम्मोहक बन गई है ।
मूर्तिकार की कला का एक ऐसा उत्तम उदाहरण है वृक्षिका या परी, जो ग्वालियर में गिरसपुर में दर्शाया गया है । जहां एक दिव्य कन्या की एक सुन्दर आकृति जो एक वृक्ष के सहारे मनोहारी रूप से टिकी हुई है, वह आभूषणों से अलंकृत है और एक महीन बनावट वाले वस्त्र से सुसज्जित है जो एक उचित रूप से सजाई गई सिल्क का आभास देता है । उसका केशविन्यास कलात्मक रूप से व्यवस्थित है । उसके माथे पर छोटे छल्ले और उसके होठों पर मन्दं मुस्कान सुन्दर महिला के आकर्षण में वृद्धि करती है । प्रतिभाशाली मूर्तिकार ने मनोहारी रूपरेखा के उत्तम चित्रण को इतनी प्रवीणतापूर्ण कौशल से छेनी की सहायता से काटा है कि हम जिसे देख रहे है वह एक खुरदरा, कठोर और भावशून्य पत्थर नहीं है बल्कि यह कोमल, जीवंत तथा स्पंदनशील रूप है ।
गुर्जर प्रतिहार एक विशाल साम्राज्य था जिसके अन्तर्गत गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता था । आठवीं, नौवीं और दसवीं शताब्दियों में इनके शासकों ने विशाल सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन देखा था । कांची के पल्लव शासकों के तत्वावधान में अत्यधिक महत्त्ववाला एक कलात्मक आन्दोलन फला-फूला था और महाबलीपुरम में सात विशालकाय पैगोडाओं का निर्माण करने का श्रेय इन्हीं शासकों को जाता है । कुछ उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इनका संरक्षण प्राप्त होने का सौभाग्य मिला था । इनमें से कुछ हैं : प्रस्तर पर उत्कीर्णन में महिषासुरमर्दिनी, गिरिगोवर्धन फलक, अर्जुन का तप या गंगा का अवतरण, त्रिविक्रम विष्णु , गजलक्ष्मी और अनन्तशयनम् । भारतीय कला के इतिहास में अर्जुन के तप वाले दृश्य में हाथी के निरूपण के अलावा संभवत कोई बेहतर उदाहरण नहीं है । स्वर्गिक विश्व, सांसारिक विश्व तथा साथ ही साथ पशुओं की दुनिया को निपुणतापूर्ण कौशल के साथ दर्शाया गया है ।
गणेश रथ के दक्षिण-पश्चिम के निकट और अर्जुन के तप के पीछे एक गुफा है जो वराहमण्डप के नाम से जानी जाती है तथा अपने आप में एक उत्कृष्ट नमूना है । अग्र भाग में स्थित सभा-भवन दो-सिंह स्तंभ और दो भित्ति स्तम्भ हैं और इसके आगे मध्य में एक कक्ष है जिसकी सुरक्षा में दो द्वारपाल तैनात हैं । पैनलों में से एक वहां का चित्रण करता है जिसने समुद्र से धरती को उठाया था तथा इसी समुद्र में वह जलमग्न हो गई थी । इसकी एक असाधारण विशेषता यह है कि वराह की तुण्ड को अत्यधिक सावधानी से निर्मित किया गया है और पशु के सिर को इतनी दक्षता से संभाला गया है कि यह पैनल की शेष आकृति की मानवीय रूपरेखा में एक प्राकृतिक ढंग से मिश्रित हो जाता है । सूर्य, ब्रह्म और देवी धरा को वराह के आसपास एवं उसे शृंगार कराते हुए दिखाया है । वराह का दाहिना पैर नागराज शेष के छत्र पर टिका हुआ है । कमल की पंखुडि़यां और पुष्प तथा उनके लहराने का चित्रण इस प्रकार से किया गया है कि यह जल का आभास देता है ।
इन सभी उदाहरणों में ओज की संरचना अद्वितीय है । पल्लव शैली की अभिरुचि एक दीर्घ और छरहरी आकृति में है । दुबले-पतले और दीर्घीकृत अंग आकृति की लम्बाई पर बल देते हैं । महिला आकृतियां अपनी छरहरी कमर, तंग स्तनों तथा कंधों, अपेक्षाकृत छोटे वक्षस्थल, छितरे आभूषण तथा वस्त्र और सामान्यत: विनम्र मुद्रा के साथ अधिक हल्की प्रतीत होती हैं । पल्लव की मूर्तिकला मुद्रा और प्रतिरूपण में स्वाभाविक है । धड़-प्रतिमा का अग्र भाग लगभग समतल है, और उच्च उभार के साथ अलंकरण साधारण है, फिर भी यह एक निश्चित मात्रा में उत्साह और प्रवाही लालित्य से परिपूर्ण है । महाबलीपुरम् का उत्कीर्णन एक महान कला-कृति है जिसमें महान देवी दुर्गा को भैंसे के सिर वाले राक्षस से एक भीषण युद्ध करते हुए दिखाया गया है तथा इनकी अपनी अपनी सेनाएं इनकी सहायता कर रही हैं । दुर्गा अपने शेर पर सवार होकर पूरे साहस के साथ शक्तिशाली राक्षस की ओर दौड़ रही हैं । राक्षस पीछे हट रहा है फिर भी वह आक्रमण करने की प्रतीक्षा में है ।
यह अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच निरन्तर संघर्ष का निरूपण करता है, जिसमें अन्तत: अच्छाई की विजय होती है । इस मूर्तिकला की नाटकीय गति, भावनात्मक प्रगाढ़ता और दृश्य यथार्थवाद एक निपुण शिल्पीकार के योग्य हैं । बाद में पल्लव मूर्तिकला कारीगरी, सुगम रचना और अधिक विकसित कलात्मक परिष्करण को अधिक गहराई से दिखाया गया है । विष्णु का ऊंचा बेलनाकार मुकुट, भारी वस्त्र, प्रमुख फंदों और फुंदनों के साथ मोटी डोरी और अन्दर पहनने वाले वस्त्रों को पहनने की रीति, ये सभी पल्लव की विशेषताएं है जिनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।
आठवीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों ने चालुक्य वंश से शक्ति छीन ली थी । इन्होंने एलोरा में अपने कैलाश मन्दिर में मध्यकालीन भारतीय कला के सबसे महान आश्चर्य का सृजन किया । एक पहाड़ी और ठोस चट्टानों से खोद कर निकाली गई इस कृति का बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया है । इस मन्दिर का सुदृढ़ तथा भव्य उत्कीर्णन, आत्मिक और शारीरिक संतुलन को प्रतिबिम्बित करते हुए, ऊंची एवं प्रभावशाली रूप से निर्मित आकृतियों की राष्ट्र कूट शैली को दर्शाता है । एलोरा में गुफा सं. 29 में भव्य वास्तुकलात्मक शैल मूर्ति शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाती है । संकोची पार्वती का हाथ पकड़े हुए शिव, कृति के मध्य में हैं । दाहिनी ओर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पवित्र अग्नि की लपटों को प्रज्जवलित करने में व्यस्त, हैं । पार्वती के माता-पिता अपनी पुत्री को महादेव को अर्पित करने के लिए पीछे की ओर खड़े हैं । इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए देवों को मुख्य आकृतियों के ऊपर लहराते हुए दिखाया गया है । दैवीय दम्पति की गौरवपूर्ण मनोहरता और इस अवसर पर समारोह की सौम्यता को मूर्तिकार ने निपुणतापूर्ण कौशल से प्रस्तुत किया है ।
कैलाश पर्वत को रावण द्वारा हिलाने के दृश्यी को प्रस्तुत करने वाला एक फलक एलोरा की एक अन्य भव्य कृति है । इस असाधारण दृश्य में पर्वत के कम्पन को महसूस किया जा सकता है । पार्वती को अत्यधिक विचलित दिखाया गया है, वे शिव की ओर देख रही हैं, उन्होंने भयवश शिव का हाथ पकड़ा हुआ है, जबकि उनकी दासी पलायन कर रही है लेकिन देवों के देव शान्त हैं और वे अपने पैर से पर्वत को दाब कर कस कर पकड़े हुए हैं । कृति का नीचे का आधा भाग यह दर्शाता है कि रावण अपने बीस हाथों से पर्वत पर अपना पूरा-पूरा जोर लगा रहा है ।
नागराज और उसकी रानी को दर्शाने वाले एक शास्त्रीय फलक का संबंध अजन्ता से है और यह पांचवीं शताब्दी ईसवी का है । इसमें इन दोनों को एक राजसिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है और एक दासी उनकी देखभाल कर रही है । अजन्ता की मूर्ति कलाकृतियां विश्व विख्यात भित्तिचित्रों की भांति अत्यधिक ध्यान देने योग्य हैं ।
वाकाटक परम्पराओं को प्रारम्भिक सातवाहन से लिया गया है जो अजन्ता में चित्रित तथा उत्कीर्ण की गई आकृतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । ऐसे मात्र सजावटी तत्त्व ही हैं जिनकी रचना मोतियों तथा रिबन से की गई हैं और गुप्त वाकाटक काल की यही विशेषता इन्हें अमरावती की सरल, लेकिन ध्यान देने योग्य, मूर्तिकला से भिन्न बनाती है । एलीफेन्टा की गुफा में तीर्थ-मन्दिर राष्ट्रकूटों का एक अन्य ऐसा महान स्मारक है जिसमें सुप्रिसिद्व महेश मूर्ति है । एक ही शरीर से उत्कीर्ण तीन सिर भगवान शिव के तीन विभिन्न पहलुओं का निरूपण करते हैं, शान्त और सम्मानित दिखने वाला मध्यवर्ती चेहरा उन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में दिखाता है, बाईं ओर का कठोर दिखने वाला चेहरा उन्हें विनाशकर्ता के रूप में चित्रित करता है और दाहिनी ओर का तीसरा चेहरा शान्त और प्रशान्त अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है ।
शक्तिशाली चोल शासकों, जिन्होंने पल्ल्व का स्थान लिया और नौंवी से तेरहवीं शताब्दी ईसवी सन् तक दक्षिण भारत में राज किया, ने तंजावुर, गंगाईकोंड चोलापुरम्, दारासुरम में प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण किया जो उनकी कला का वास्तव में तोशखाना थे । चोल मन्दिरों में सर्वाधिक परिपक्व तथा राजसी मन्दिर तंजावुर का बृहदीश्वर मन्दिर है जिसकी मूर्ति ने एक नवीन परिपक्वता हासिल कर ली हैं जो कि मूर्तियों की मनोहारी ढंग से चित्रित रूपरेखाओं, उनकी नियत मुद्राओं, उत्तम अलंकरण, भव्य चेहरों और कुछ जीवंतता में स्पंष्ट हो जाती है और ये सब मिलकर कलाकृति की सौम्यता में वृद्धि करते हैं । चोल कला ने न केवल लंका की कला को प्रभावित किया बल्कि यह जावा और सुमात्रा तक भी पहुंच गई थी।
ग्यारहवीं शताब्दी में चोल शिल्पकारी का एक अच्छा उदाहरण गजासुरसंहारमूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्णन है । क्रुद्ध महादेव उस हाथी-राक्षस का, जिसने ऋषियों और उनके भक्तों को बहुत प्रताडि़त किया, संहार करने के पश्चात भीषण हर्षोन्माद के एक ओजस्वी नृत्य में व्यस्त हैं । राक्षस के छिपने का स्थान महादेव के ऊपर फैला हुआ है । आवरण के लिए महादेव राक्षस की खाल हाथ से ऊपर उठाएं हुए हैं । प्रतिशोध के इस दिव्य कृत्य के एकमात्र विस्मयाकुल दर्शक के रूप में देवी निचले दाहिने कोने पर खड़ी हैं ।
तेरहवीं शताब्दी में चोल कला के उत्तरवर्ती चरण में भूदेवी को विष्णु की कनिष्ठ पत्नी के रूप में दर्शाकर मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है । वे एक कमल के आधार पर आकुंचित मुद्रा में मनोहारी रूप में खड़ी हैं, उनके दहिने हाथ में कुमुदिनी का एक पुष्प है और बायां हाथ लोलाहस्त में उनके पार्श्व में है ।
चन्देल शासक जिन्होंने 950 से 1100 ईसवी सन् तक शासन की बागडोर संभाली, ने मध्यभारत में बहुत ऊंचे मन्दिरों का निर्माण किया यथा खजुराहो में कंदरिया महादेव मन्दिर । इन मन्दिरों का निर्माण में अन्तहीन विविधता वाली मानव मूर्तियों से किया गया था । यहां मूर्तिकार ने रेखीय ब्योरों के पर्याप्त जोर के साथ छरहरी तथा लम्बी आकृतियों को वरीयता दी है ।
ग्यारहवीं शताब्दी की चंदेल कला का एक मनोहारी नमूना एक ऐसी महिला की आकृति है जो प्रेम पत्र लिख रही है । उसके दाहिने कंधे के पीछे उंगली के नाखूनों के चिह्न हैं जो उसके प्रेमी ने उसे आलिंगनबद्ध करते समय लगा दिए थे । अपने प्रेमी से मिलने के दौरान अनुभव किए गए आनन्द का स्मरण करते हुए और उससे पुन: मिलने की इच्छा करते हुए वह यह प्रेम पत्र लिख रही है । उसके दूसरी ओर उसकी एक परिचारिका खड़ी है ।
आम के सुरुचिपूर्ण वृक्ष के नीचे खड़ी हुई एक मनोहारी स्वर्गिक महिला को दर्शाने वाली कृति समान रूप से आकर्षक है । उसके हाथ में दर्पण है, वह शृंगार कर रही है और अपने प्रेमी से मिलने के लिए तैयार हो रही है । दो अल्प आकृतियां हाजिरी में खड़ी है और उन्होंने एक थैले तथा बस्ते में प्रसाधन संबंधी आवश्यक सामग्री रखी हुई है । यह मूर्ति ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी की है । कल्पना की भव्यता तथा सम्पूर्णता और खजुराहो में मूर्तिकला की प्रचुरता भारतीय कला में उत्कृष्ट है । देव, देवियां, अप्सराएं, पुरुष और महिलाएं अपने सुविकसित विलासमय शरीर के साथ खड़ी हुई हैं, कुछ करती हुई प्रतीत होती हैं । अपने फ्रेम से बाहर निकल कर स्वतंत्र रूप से खड़ी हैं ताकि वे अपने स्वयं के जीवन्त विश्व में ऊपर उठ सकें । खजुराहो की कला सौन्दर्य की एक दुनिया है । आलिंगनबद्ध प्रेमी-प्रेमिका जिन्हें लगभग उत्कीर्ण करके बनाया गया है, गुंजित मनोवेग को प्रदर्शित करते हैं । मुस्कुराहट में थोड़ा-सा परिवर्तन करके, अभिव्यक्ति में तथा थोड़ा-सा अन्तर ला कर मुद्रा में विभिन्न प्रकार के मनोभावों को लाया जाता है । खजुराहो की मूर्तियां भारतीय मूर्तिकला की इतनी महान कला-कृतियां हैं कि इनकी अलग-अलग तथा साथ ही साथ संचयी रूप में सराहना की जा सकती है ।
730 से 1110 ईसवी सन् की अवधि के दौरान बिहार और बंगाल में पाल शासकों के शासनकाल में कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया था । इनका बौद्ध धर्म में विश्वास था । इन्होंने नालन्दा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा-प्राप्ति के ऐसे केन्द्रों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जहां स्तूपों और मठों ने मूर्तिकार की कला की अभिव्यक्ति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया और जिसे धर्म में प्रेरणा मिली । इस अवधि के दौरान कला को तकनीकी सम्पूर्णता मिली । छरहरी और मनोहारी आकृतियां, पर्याप्त आभूषण तथा परम्परागत सजावट पाल शैली की विशेषताएं हैं । बिहार से इनकी मूर्तियां बंगाल की तुलना में अंगों के अपने सामान्य अनुपात में कुछ अधिक मोटी तथा भारी हैं । पाल शासकों के जावा के साथ घनिष्ठ संबंध थे तथा यह हिन्दू जावाई मूर्तिकला, तथा नेपाल, कश्मीर, बर्मा एवं थाईलैण्ड की चित्रकला से स्पष्ट भी होता है ।
पाल कला के उत्तरवर्ती चरण में रूढ़ अंकन कुछ मात्रा में देखा गया है, लेकिन यह परम्परा बारहवीं शताब्दी में सेन शासकों की अधीनता से लेकर देश में इस्लामी शासकों द्वारा फैल जाने तक जारी रही । पश्चिम बंगाल में महानद में एक उत्कृष्ट नमूना नदी की देवी गंगा की सुन्दर आकृति है । वे कल्पतरु, वृक्ष के नीचे एक कमल के पुष्प पर मनोहारी ढंग से खड़ी हुई हैं तथा उनके हाथ में समृद्धि और प्रचुरता की प्रतीक जल-पात्र कड़ी हुई है । उनके दुपट्टे के सिरे हाथों पर लिपटे हुए हैं और यह दोनों ओर फैला हुआ है । इन्हें पर्याप्त आभूषणों से सजाया गया है तथा इन्होंने एक आधा वस्त्र पहना हुआ है जो टखनों तक जा रहा है । आकृति सार्थक है और कारीगरी उच्च स्तर की है ।
सातवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच ओडिशा में पूर्व गंगा राजवंश के राजाओं ने अपना प्रभाव छोड़ा था तथा ये अपने पीछे भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के विशाल मन्दिर छोड़ कर गए हैं जो मूर्तियों की सम्पदा से समृद्ध रूप से सजे हुए हैं ।
नौवीं शताब्दी ईसवी सन् के मध्य तक विशेष रूप से ओडि़शा में, मूर्तिकला की एक शैली का विकास हुआ जिसने अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के सौन्दर्यपूर्ण रूपों में इंद्रियगत आनन्द प्रदान किया । दीवारों के अग्रभाग में सुन्दर महिला आकृतियों की असंख्य मूर्तियां हैं ।
ओडि़शा के मन्दिर में मनोहारी और युवा की सम्मोहक मुस्कान, राजसी आभूषणों से सजे केशों के साथ ऐसे कई प्रतिमाएं हैं, जिन्हें नायिका कहते हैं । यहां समान रूप से सुन्दर, कम वस्त्र धारण किए हुए, लेकिन कमरबन्द, कंगन, बाजूबन्द, कंठी, कर्णफूल और केश आभूषणों के बाहुल्य के साथ अन्य कृतियां हैं । ऐसी ही सुन्दर महिलाएं हर जगह प्रकट होती हुई दिखाई देती हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्षों एवं लताओं में से स्वयं सुन्दर फूलों तथा बेलों के समान निकल रही हैं । इन्होंने प्राय: वृक्षों की शाखाओं को पकड़ा हुआ है और पुष्प आभूषणों पर खड़ी हुई हैं । ये परियां और वनदेवी हैं जो वृक्षों तथा झाडि़यों में रहती हैं तथा इनमें जीवन का संचार करती हैं । पूर्ववर्ती नमूनों से ये इस दृष्टि से भिन्न हैं कि इस युग में ये उत्कृष्ट रूप से सौन्दर्यपूर्ण कन्याएं बन गई हैं, ये अधिकांशत: अल्प वस्त्रों में और कभी-कभी तो निर्वस्त्र भी होती हैं । इन्हें ओडि़शा तथा मन्दिरों की सजावट करते हुए दिखाया गया है जो अलंकरण का एक विशाल वन बन जाता है, फूलों एवं बेलबूटों की जहां भरमार है और जिसका एक रमणीक ज्यामिति अभिकल्प है । इन भव्य महिलाओं में से अधिकांश नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में खड़ी हुई हैं ।
12वीं शताब्दी के मध्य में कोणार्क के प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण नरसिंहबर्मन ने किया था । यह सूर्य को समर्पित है । इसकी कल्पना विशाल पहियों पर पत्थर के एक विशाल रथ के रूप में की गई है, जिसे पिछले पैरों पर खड़े सात अश्व खींच रहे हैं । यह मन्दिर आंशिक रूप से संरक्षित है । इसके पीठासीन देवता, सूर्य भगवान को उत्तर भारत की प्रतीकात्मक शैली में दिखाया गया है जिन्होंने पादुकाएं, जिरह-कवच पहना है, प्रत्येक हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है । वे एक रथ पर सवार हैं, जिसे सात अश्व खींच रहे हैं । दोनों ओर उनकी दो पत्नियां छाया तथा सुवर्चसा हैं तथा परिचारिकाएं दण्डा एवं पिंगल हैं । ऊपरी सिरे पर बनी आकृतियां अंधेरे को दूर करने के लिए तीर चला रही हैं ।
मन्दिर के जगमोहन की धरती से लगभग 50 फुट की ऊंचाई पर, सभी दिशाओं की ओर अभिमुख विशाल और स्वदर्गिक संगीतकार विराजमान हैं जो अलग-अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं । ये अविवाहित कन्याएं वीणा बजाते हुए दिखाई गई हैं । इस आकृति के विशाल आयाम तथा शक्तिशाली प्रतिरूपण, और इसके चहरे पर हल्की-सी मुस्कान सद्भावपूर्ण आनन्दं की एक भावना को अभिव्यक्त करती है ।
वीणा वादक के ही समान एक अन्य स्वीर्गिक अविवाहित कन्या, यह मृदंग बजा रही है । ये सभी मूर्तियां एक अपरिष्कृत बनावट में गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर की हैं । ये आकृतियां विशालकाय हैं लेकिन फिर भी इन्हें अति सुरुचिपूर्ण तथा सुन्दर ढंग से उत्कींर्ण किया गया है ।
इसके अतिरिक्त गम्भींर दृश्य भी हैं जिसमें एक गुरु को जीवन से भरपूर स्थिति में, अपने शिष्यों से घिरे हुए दिखाया गया है ।
कोणार्क मन्दिर के महान निर्माता नरसिंह को अपने अन्त:पुर में सुन्दर महिलाओं से घिरे हुए, संगीत सुनते हुए एक झूले पर दिखाया गया है ।
एक अन्य दृश्य में इनके ही संरक्षण में आयोजित कवियों की एक सभा में इन्हें साहित्य की सराहना करते हुए दिखाया गया है । जबकि एक अन्य दृश्य में इन्हें शिव, जगन्नाथ और दुर्गा के समक्ष धर्मों के प्रति सहिष्णुता प्रस्तुत करते हुए दिखाया गया है । कोणार्क में इनके जीवन और समृद्ध मूर्तिकला के अनेक अन्य निरूपण हैं जिन्हें ओडिशा में तेरहवीं शताब्दी की संस्कृति के भण्डार-गृह के रूप में समझा जा सकता है ।
कोणार्क में सूर्य मन्दिर के सूर्य की आकृति को पिछले पैरों पर खड़े सात अश्वों द्वारा खींचा जा रहा है, जिनमें से एक पूर्णरूपेण सुसज्जित है । यह मन्दिर विशाल आनुपातिक आकृति का है ।
ओडिशा के कारीगरों ने मनोहरता तथा ओजस्विता की परम्परागत पद्धतियों को छोड़े बिना ही ऐसी आकृतियों का निर्माण किया जो अपने रूप और जीवन-शक्ति की सम्पूर्णता में दोषरहित थीं । इस शैली के उदाहरणों में इन्द्रियगत सौम्यता और रूप में सुन्दरता थी । मिथुन अथवा कामासक्त प्रेमी-प्रेमिका की एक जोड़़ी, ओडि़शा की कला की प्रचुर विशेषताओं के साथ दमकती है । इनमें ऐसे प्रेमियों की शाश्वत मुस्कान है जो एक-दूसरे में विलीन हो गए हैं । समय-समय पर तथा साथ ही साथ तकनीक की दृष्टि से, ओडिशा की कला कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर के रूप में पराकाष्ठा को प्राप्त हुई है ।
पश्चिमी भारत में गुजरात की संगमरमर मूर्तिकला की परम्पराओं को जटिल रूप से उत्कीर्ण की गई मूर्तियों के रूप में प्रचुर मात्रा में देखा जाता है जो माउंट आबू गिरनार और पालीताणा के जैन मन्दिरों को सजाती हैं । हिन्दुओं की सुरक्षा के देव चार भुजाधारी विष्णु की सुन्दर प्रतिमा इनकी गदा, चक्र और शंख जैसी विशिष्ट विशेषताओं के साथ तेरहवीं शताब्दी ईसवी में बनाई गई थी । कमल के पुष्पी को धारण करने वाली भुजा अब गुम हो गई है । शास्त्रों के आधार पर पुन: साकार अनुषंगी आकृतियों के रूप में दिखाया गया है । दोनों ओर परम्परागत सजावटी मूलभाव और आयाताकार आलों के भीतर ब्रह्म तथा शिव की लघु प्रतिमाएं दिखाई देती हैं । माउंट आबू में दिलवाड़ा मन्दिर जैन परम्परा की पश्चिमी शैली की उत्कृष्ट कृति हैं । ये वास्तुकला की स्मारक तो नहीं है लेकिन मूर्तिकला की उत्कृष्ट कला-कृतियां अवश्य हैं तथा एक-दूसरे के ऊपर संजोई हुई हैं ताकि विश्व की आश्चर्यजनक मूर्तियों में से इन्हें एक में देखा जा सके । दिलवाड़ा मन्दिर की छत विशेष रूप से सूक्ष्मता से उत्कीर्ण मूर्तिकला विश्व की उत्कृष्ट कला-कृतियों में से एक है ।
होयसल दक्षिण भारत का एक अन्य राजवंश था जिसने बारहवीं शताब्दी के लगभग प्रारम्भ में मैसूर क्षेत्र में स्वयं को शामिल किया । उन्होंने हेलीबीड और बेलुर में जिन मन्दिरों का निर्माण किया वह पत्थर में जालीदार कार्य के समान प्रतीत होते हैं । मानव शरीर की गति या मनोरमता की तुलना मे अलंकरण पर अधिक बल दिया गया है। होयसाल की मूर्तियां कुछ गोल-मटोल तथा छोटी हैं, अत्यधिक अलंकृत है या आभूषणों से अधिक लदी हुई हैं लेकिन देखने में फिर भी मनोहारी प्रतीत होती हैं ।
इस समय तक हम अपनी यात्रा की समाप्ति के अति निकट पहुंच गए हैं और हमने यह पाया कि तेरहवीं शताब्दी ईसवी सन् में मानव आकृति के सौन्दर्य के प्रति प्यार पूर्णरूपेण समाप्त हो गया था । अब कलाकार को मनोहार पुरुष या प्रीतिकर महिला के शरीर की सुन्दरता को चित्रित करने में आनन्द की अनुभूति नहीं होती थी । इसके विपरीत सजावट तथा अलंकरण के एक विलक्षण अम्बार जो कि मानव शरीर से अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया था, के नीचे मानव शरीर कहीं लगभग लुप्त हो गया था ।
इस समय की मूर्तियों में एक महिला की मूर्ति को चंवर पकड़े हुए दर्शाया गया है और अन्य आकृतियों में हम शरीर को लगभग लुप्त पाते हैं । इससे कुछ शताब्दी पूर्व, महिला की लहरदार घुमावों वाली सुन्दर आकृति का गुणगान किया गया होगा, अब उस सौन्दर्य का कुछ भी नहीं बचा है । वास्तव में अलंकरण हावी हो गया है । करमबंद, मुकुट, बाजूबन्द और कंगन और यहां तक कि उसके पीछे तथा ऊपर का वृक्ष भी वस्त्रों के आकर्षक बेलबूटेकार की नक्काशी में परिवर्तित हो गया है ।
दक्षिण भारत में अन्तिम महान हिन्दू साम्राज्य विजयनगर था । लगभग 1336 से 1565 ईसवी सन् तक इस शासनकाल में, ताडपत्री, हम्पी, कांचीपुरम् आदि जैसे स्थानों पर अनेक सुन्दर मन्दिरों का निर्माण किया गया था । इन मन्दिरों के उत्कीर्णन चोल और चालुक्य परम्पराओं को दर्शाते हैं । इस अवधि के दौरान रामायण और कृष्ण बाल लीला का वर्णनात्मक रूपों में निरूपण लोकप्रिय विषय बन गया था । विजयनगर सम्राटों ने मूर्तिकारों से उत्कृष्ट प्रतिकृतियां उत्कीर्ण करवाई ताकि उन्हें आराध्यक देवताओं के सामीप्य में अमर बनाया जा सके ।
चिदम्बरम में एक गोपुरम् में कृष्णदेवराय एक उत्तम उदाहरण है । इसका अन्तिम स्फुरण तिरुमलनायक और गोपुरम् और मदुरै के मीनाक्षी मन्दिर के परिसरों में मूर्तिकारों द्वारा भीमकाय आकार में उत्कीर्ण की गई विस्मयकारी एवं ओजस्वी मूर्तियों को देखा जा सकता है ।
सत्रहवीं शताब्दी मदुरै और तंजावुर के नायक के अधीन भीमकाय कला-कृतियों का एक महान युग था । इस अवधि के दौरान, त्रिचिनापल्ली में श्रीरंगम मन्दिर की उत्कृष्ट मूर्तिकला में विलक्षण वर्णन के साथ पशुओं की मूर्तियों को देखा जा सकता है । हालांकि यह कला रूढ़ है, फिर भी यह ऊर्जा से परिपूर्ण है । उच्छृंखल, उन्मत घोड़ों का एक जोड़ा, जिसका सिर खम्भों को सहारा प्रदान करता है, अति कुशलता और उत्साह से उत्कीर्ण किया गया है । सवार यथार्थवादी मुद्राओं में दिखाए गए हैं, जो उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं । प्रत्येक मूर्ति वास्तविक है, जबकि संकल्पना विलक्षणकारी है ।
हालांकि पत्थर मूर्तियों के सृजन करने की परम्परा जारी रही, मुगलों और अन्य मुसलमान शासकों के अधीन मूर्तिकला का कोई भी प्रमुख आन्दोलन जीवित नहीं रह सका । मुसलमान शासकों के अधीन वास्तुकला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया था लेकिन मूर्तियां विरल ही पाई जाती हैं और यहां तक कि जो उपलब्ध भी हैं वे स्थानीय नायकों की देन हैं । ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मूर्तिकारों को कोई समुचित संरक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया था और भारतीय कला की समूची परम्परा को विराम लग गया था ।